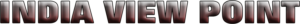सुंदर दिखने की इच्छा इंसान में आदिम युग से ही मौजूद रही है। प्रारंभिक मानव समाजों में साथी चुनने के लिए आकर्षक, स्वस्थ और प्रजनन-सक्षम शरीर को प्राथमिकता दी जाती थी। इसलिए सुंदरता को जीवन और वंश की निरंतरता से जोड़ा गया। यह प्रवृत्ति जैविक थी, लेकिन जैसे-जैसे सभ्यताएं विकसित हुईं, सुंदरता का विचार सांस्कृतिक और सामाजिक दबाव में बदल गई, जहां सुंदरता को सम्मान, स्वीकृति और सफलता से जोड़ दिया गया। कालांतर में समाज ने सुंदरता के अपने मानक मसलन गोरा रंग, पतली काया, लंबे बाल आदि तय कर दिए।
इन मानकों ने स्त्रियों पर विशेष रूप से दबाव डाला और सुंदरता को उनकी “मूल्यवत्ता” का आधार बना दिया। आधुनिक दौर में मीडिया और बाज़ारवाद ने इस चाह को और गहरा कर दिया, जिससे सुंदरता अब आत्म-संतोष की नहीं, बल्कि सामाजिक मान्यता पाने की ज़रूरत बन गई है। विज्ञापन, फिल्में और सोशल मीडिया ने तो सुंदरता को व्यापारिक वस्तु बना दिया। अब सुंदर दिखने की इच्छा अक्सर आत्म-संतोष नहीं, बल्कि सामाजिक स्वीकृति, सराहना और सफलता पाने की मजबूरी बन चुकी है। यह चाह अब स्वतंत्र नहीं, बल्कि थोपी हुई है।
दूसरे शब्दों में कहें तो हर इंसान किसी न किसी को इम्प्रेस करना चाहता है। इसलिए आकर्षक और कम उम्र का दिखना चाहता है। लेकिन ख़ूबसूरत, आकर्षक और कम उम्र का दिखने की भी एक सीमा होती है। क्योंकि मानव के पास महज़ 60 या 70 साल या फिर 80 साल का ही जीवन है। जो ज़्यादा फिज़िकली स्वस्थ हैं तो संभव है वह 90 साल तक जी लें। लेकिन व्यवहारिक रूप से अस्सी के बाद के जीवन को जीवन नहीं बल्कि घसीटना कहा जाता है। इस जीवन से दूसरों को असुविधा होती हैं। कुछ लोग इस असुविधा का ज़ाहिर कर देते हैं और कुछ लोग परंपरावश ज़ाहिर नहीं कर पाते है।
इसलिए आप मान लीजिए कि आपको जो कुछ भी करना है उसे इतने साल में कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद सांसारिक चीज़ें तो दूर आपका अपना शरीर ही आपका साथ नहीं देने वाला है। यही सच है और यह फ़लसफ़ा हर इंसान को समझ लेना चाहिए। जैसे बचपना के बाद तरुणाती आती है वैसे ही तरुणाई के बाद बुढ़ापा आता है। इसलिए किसी के अंदर सुंदर या कम उम्र का दिखने की सनक नहीं होनी चाहिए। यह सनक अप्राकृतिक है। हर अप्राकृतिक कार्य का लाभ बहुत कम लेकिन नुक़सान बहुत ज़्यादा होता है। अप्राकृतिक कार्य करने वाले का कभी-कभी इतना नुक़सान हो जाता है कि उसकी जान ही चली जाती है।

‘कांटा लगा’ अभिनेत्री शेफ़ाली ज़रीवाला इसी सनक के चक्कर में जान गंवा बैठीं। अगर कम उम्र की दिखने का उफक्रम न करती तो शायद 70-80 साल जी लेतीं लेकिन कम उम्र की दिखने के लिए अपनाए गए अप्राकृतिक तरीक़ों के कारण दुर्भाग्यवश वह 42 की उम्र में ही इस दुनिया से चल बसीं। उनकी मौत के बाद इस तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर ख़ासा चर्चित है, क्योंकि वह एंटी-एजिंग मेडिसीन लेती थीं। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों का कहना है कि एंटी-एजिंग मेडिसीन के रिएक्शन से ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। हालांकि इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
शेफ़ाली का ग्लैमर, उनकी स्टाइल और आत्मविश्वास ने उन्हें एक पॉप कल्चर आइकन बना दिया। लेकिन वक्त के साथ जैसे-जैसे उम्र बढ़ी, लोग उन्हें उनके टैलेंट से ज़्यादा उनकी स्किन, उनकी बॉडी और उनके लुक्स से आंकने लगे।
कई इंटरव्यूज़ में शेफाली ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने “फेशियल ट्रीटमेंट्स”, “स्किन प्रोसिजर्स” जैसी चीज़ों का सहारा लिया ताकि वे ‘उम्र का असर’ अपने चेहरे पर दिखने न दें। हालांकि वह यह भी कहती हैं कि ये निर्णय उन्होंने अपने लिए लिए, लेकिन क्या यह सच में उनका अपना निर्णय था, या उस अदृश्य सामाजिक दबाव का असर जिससे आज हर उम्रदराज़ महिला जूझ रही है?
सवाल यह है कि क्या आज के बाज़ारवादी दौर में स्त्रियों पर कम उम्र और सुंदर दिखने का वाक़ई सामाजिक दबाव होता है? इन दिनों यह सवाल तेजी से उभर रहा है कि क्या स्त्रियां इसलिए सुंदर दिखना चाहती हैं, क्या स्त्री मान चुकी है कि वह वस्तु हैं, और सुंदर वस्तुओं के ग्राहक अधिक होते हैं? यह प्रश्न केवल सौंदर्य की चाह तक सीमित नहीं है, बल्कि स्त्री की सामाजिक स्थिति, आत्म-अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता और सांस्कृतिक दबावों की गहरी परतों को भी उजागर करता है।
सौंदर्य की अवधारणा में स्त्री की भूमिका
ऐतिहासिक रूप से स्त्रियों को “सज्जा की वस्तु” के रूप में देखा गया है। चाहे वह शाही दरबार हों या आधुनिक फ़िल्मी पर्दा, स्त्री का सौंदर्य ही उसका मूल्य तय करता रहा है। “सुंदर कन्या” होना विवाह के बाज़ार में स्त्री की “बिक्री” की गारंटी समझा जाता है। यह सौंदर्य केवल चेहरे या शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि व्यवहार, पहनावे, चाल और आवाज़ तक विस्तारित हो चुका है। जब समाज किसी स्त्री को उसकी क्षमताओं, विचारों या संवेदनशीलता से पहले उसके रूप से आंकने लगता है, तो यह स्वाभाविक हो जाता है कि वह स्वयं को एक वस्तु की तरह सजाने-संवारने लगती है।
मीडिया और सौंदर्य का बाज़ारवाद
विज्ञापन, फ़िल्में, सोशल मीडिया और सौंदर्य उद्योग ने मिलकर स्त्री को एक ‘ब्रांडेड पैकेज’ बना दिया है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि “अगर आप सुंदर दिखेंगी, तो आप सफल होंगी, चाही जाएंगी, सराही जाएंगी।” इस सोच ने सौंदर्य को एक उत्पाद बना दिया है और स्त्री को उसका उपभोक्ता भी और प्रदर्शनकर्ता भी। फ़ेयरनेस क्रीम से लेकर स्लिमिंग सेंटर तक और हाई-हील्स से लेकर मेकअप ट्यूटोरियल तक—हर जगह यही सन्देश है: “तुम जैसी हो, वो पर्याप्त नहीं है। तुम्हें और सुंदर बनना होगा।”
क्या यह सौंदर्य की स्वतंत्र चाह है?
यह तर्क अक्सर दिया जाता है कि हर स्त्री को सुंदर दिखने का अधिकार है। बिल्कुल है। लेकिन जब यह “अधिकार” दरअसल सांस्कृतिक अनिवार्यता बन जाए, तब यह स्वतंत्रता नहीं, बल्कि परोक्ष गुलामी बन जाती है। क्या स्त्रियां सचमुच इस दबाव के बगैर भी सजना चाहती हैं? या वे इसलिए सजती हैं क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया कि उनकी ‘कीमत’ उनकी सुंदरता में है? यहां यह समझना आवश्यक है कि सौंदर्य की चाह और सौंदर्य की मजबूरी में बारीक फर्क है।
क्या स्त्री का अर्थ वस्तु है?
स्त्रियों को वस्तु की तरह देखे जाने की यह सोच उन्हें केवल समाज की नज़र में नहीं, बल्कि उनके अपने आत्मसम्मान में भी प्रभावित करती है। जब कोई स्त्री यह मान लेती है कि सुंदर दिखना उसकी पहली ज़िम्मेदारी है, तो वह अनजाने में अपने अस्तित्व को एक “प्रोडक्ट” के रूप में देखने लगती है—जिसे रोज़ निखारना, सजाना और प्रस्तुत करना ज़रूरी है। इससे न केवल मानसिक तनाव और असंतोष उत्पन्न होता है, बल्कि कई बार डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, आत्म-तिरस्कार और आत्महत्या जैसे गंभीर परिणाम भी देखने को मिलते हैं।
सौंदर्य की इच्छा के विरोध में नहीं
यह लेख सौंदर्य की इच्छा के विरोध में नहीं है, बल्कि उस सामाजिक, सांस्कृतिक और बाज़ारवादी दबाव के खिलाफ़ है जिसने स्त्री को सौंदर्य की परिभाषाओं में कैद कर दिया है। जरूरी यह है कि स्त्रियां खुद तय करें कि वे क्यों सज रही हैं, स्वयं के लिए, आत्मसंतोष के लिए, या समाज को प्रसन्न करने के लिए? जब तक यह अंतर स्पष्ट नहीं होगा, तब तक सुंदरता की स्वतंत्रता असल में सौंदर्य की दासता ही बनी रहेगी।
अतं में यही कहना होता कि स्त्रियों की सुंदरता की चाह अगर उनके व्यक्तित्व की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, तो वह सशक्तिकरण है। लेकिन यदि यह चाह समाज द्वारा गढ़ी गई भूमिकाओं, बाजार के दबावों और स्वीकृति की मजबूरी से उत्पन्न हो, तो यह चिंता का विषय है। समाज को ज़रूरत है इस प्रश्न से मुठभेड़ करने की कि हमारी बेटियां क्या वाकई खुद को मनुष्य नहीं, वस्तु समझने लगी हैं? अगर हां, तो यह समय है उस सोच को बदलने का — कि स्त्री की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका चेहरा नहीं, उसका चेतन स्वरूप है।
इसे भी पढ़ें – सॉरी पापा, सब कुछ खत्म हो गया — दहेज प्रताड़ित रिधन्या की दर्दनाक दास्तां
Share this content: