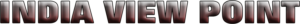ईमानदारी से कहूं तो मेरे मां-बाप ने केवल मज़े लेने के लिए सेक्स किए थे और मैं पैदा हो गया। लिहाज़ा, मेरे पैदा होने में न तो मेरा कोई योगदान था और न ही मेरा कोई वश। जहां और जिस हाल में मेरे मां-बाप रहते थे, मैं वहीं पैदा हो गया। इस देश, या कहें ब्रह्मांड के हर प्राणी की तरह, मेरे भी पैदा होने पर मेरा किसी तरह का नियंत्रण या मेरी इच्छा नहीं थी। मेरा ज़रा भी नियंत्रण होता या मेरी ज़रा भी इच्छा होती, तो ऐसा जीवन जीने के लिए मैं पैदा ही न हुआ होता। पैदा होने से ही इनकार कर देता। बोल देता, “आप ग़रीब हैं, आपके यहां पैदा होकर जीवन भर रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके यहां पैदा होने से साफ़ इनकार करता हूं।” परंतु पैदा होने पर मेरा कोई वश नहीं था। लिहाज़ा, किसी द्वारा पैदा कर दिए जाने के बाद अब अपना पूरा जीवन, 30-40, 50-60, 70-80 या 90-100 साल, जो भी हो, जीने के लिए अभिशप्त हूं। क्योंकि मैं मजदूर हूं।
अवांछित रूप से पैदा होने का यह अभिशाप ही मुझे फ़िलहाल उस जगह ले जा रहा था, जहां कोरोना वायरस के संक्रमण काल में कम से कम दो जून की रोटी के मिलने की संभावना मौजूदा जगह से शर्तिया अधिक है। और ज़ाहिर तौर पर वह जगह है, मेरा गांव, जहां मैं या मेरे बाप-दादा पैदा हुए थे। वही गांव, जहां संकट के समय ज़िंदा रहने की संभावना सबसे अधिक होती है, क्योंकि अन्न केवल उस गांव के खेतों में पैदा होता है। जिस अन्न को खाकर हर इंसान ज़िंदा रहता है।
वही गांव, जहां पहले केवल और केवल भाई-चारा और प्रेम का बसेरा रहता था, लेकिन जवाहर रोजगार योजना और मनरेगा जैसी पैसे बनाने वाली योजनाएं शुरू होने के बाद, उस भाई-चारे और प्रेम की जगह राजनीति ने ले ली है। वही गांव, जो सदैव दीन-हीन हाल में ही रहा। फिर भी वह गांव शहर के मुक़ाबले भोजन देने में अधिक उदार है। गांव में सरवाइवल फॉर द फीटेस्ट, सरवाइवल फॉर द रिचेस्ट और सरवाइवल फॉर द लकिएस्ट का फॉर्मूला लागू नहीं होता। गांव में सरवाइवल फॉर द ऑल का नियम चलता है। इसलिए केवल मैं ही नहीं, बल्कि, मेरे जैसे सभी के सभी मजदूर बस अपने-अपने गांव भागे चले जा रहे हैं।
दरअसल, मैं कोरोना महामारी और उसके असली असर को समझ ही नहीं पाया। इसलिए जब कहा गया कि ताली बजाओ तो मैंने ताली बजाई। जब कहा गया कि लाइट बुझाकर दीप जलाओ तो मैंने दीप जलाया। जब कहा गया कि लॉकडाउन है, घर में ही रहो, तो मैं घर में क़ैद हो गया। जब पहली बार लॉकडाउन की घोषणा हुई, तो मुझे लगा हफ़्ते-दो हफ़्ते की बात है। वक़्त किसी तरह गुज़ार लूंगा। जो कुछ घर में है, उससे ही काम चला लूंगा। लेकिन जब महीना बीत गया। दूसरा महीना शुरू हो गया। पैसे ख़त्म होने लगे, राशन ख़त्म होने लगा और ऊपर से मकान मालिक किराया मांगने लगा, तो मैं हतप्रभ रह गया। मुझे पहली बार लगा कि मैं तो फंस गया। फंस क्या गया, मैं तो बुरी तरह फंस गया। क्या करूं अब, यह लॉकडाउन तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है।
जैसे-जैसे राशन कम होता गया, वैसे-वैसे मेरी बदहवाशी बढ़ती गई। बाद में मेरी हवाइयां उड़ने लगीं। दिमाग़ ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया। इधर-उधर मदद के लिए देखने लगा। लेकिन मदद का कोई भी हाथ मेरी ओर नहीं आया। टीवी पर सुना कि शहर में राशन बंट रहा है। बाहर निकला, इधर-उधर गया। पर कुछ नहीं दिखा। मतलब, राशन लेने का मेरा नंबर आया ही नहीं। पूरे शहर में बंदर-बांट मची थी। हर जगह “उन्हीं को मौत की कीमत मिल रही थी, जिन पर नेता-हाकिम मेहरबान थे” का आलम पसरा था।
मुझे लगा, यहां रहूंगा तो कोरोना से भले बच जाऊं, पर भूख तो शर्तिया मुझे मार डालेगी। बस सोचने लगा, अपने गांव जाने की। गांव ही एकमात्र वह जगह है, जहां मैं कोरोना से बचने के बाद ज़िंदा रह सकता था। बस मकान मालिक से बचकर किसी तरह घर से निकल लिया। बाहर हज़ारों लोगों की भीड़ थी। थोड़ी तसल्ली हुई कि अकेले नहीं हूं। जो सबका होगा, वही मेरा भी होगा। हम लोग जिधर निकलते थे उधर ही रोका जाता था। कहीं-कहीं हम पर लाठीचार्ज भी हो रहा था। फिर भी हम लोग आगे बढ़ते रहे। कहीं मुर्गा बनना पड़ा तो मुर्गा बन गए। लाठी खानी पड़ी तो लाठी खा लिए, लेकिन चलते रहे।
मेरे साथ हर तरह के लोग थे। भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। जो भाग्यशाली थे, उनको ट्रेन मिल गई। जो कुछ कम भाग्यशाली थे, उनमें से कुछ को टैक्सी मिल गई, तो कुछ ऑटोरिक्शा से चले गए। जो और कम भाग्यशाली थे, वे अपनी या दूसरे की मोटरसाइकल से ही चले गए, जबकि कुछ साइकल से ही निकल लिए। जो लोग सबसे कम भाग्यशाली थे, उन्हें ट्रक या टैंपों में ठूंस दिया गया। और जो लोग बिल्कुल भाग्यशाली नहीं थे, वे अकेले या परिवार समेत पैदल ही चले जा रहे थे। मैं भी बिल्कुल भाग्यशाली नहीं था, सो दुर्भाग्यशाली लोगों के साथ पैदल ही चला जा रहा था। पैदल जाना ही मेरी नियति थी। हम सबकी नियति थी।
रास्ते में यदा-कदा समाजसेवा करने के शौक़ीन लोग मिल रहे थे। कोई हम बदनसीबों को पानी दे दे रहा था, तो कोई खाने की कोई चीज़। खाने-पीने की चीज़ों पर हम बदनसीब लोग टूट पड़ते थे। यह भूल जाते थे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। रोटी की मांग या मजबूरी के आगे दरअसल, सारी प्राथमिकताएं गौण हो जाती थीं। यहां भी लक्ष्य था, कुछ खाने की चीज़ हाथ में आ जाए। इस छीना-झपटी में कुछ खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते थे, जो बचते थे, उसे हम मजदूर अपने पेटों में ठूंस लेते थे। और, फिर आगे चल देते थे।
दरअसल, हम उस समाज में पैदा हो गए थे, जहां सेक्स को ही गंदी चीज़ माना जाता है। सेक्स को चरित्र से जोड़ा जाता है। यानी किसी ने सेक्स कर लिया तो चरित्रहीन हो गया या हो गई। महिलाओं के लिए तो बक़ायदा ‘कुलटा’ शब्द खोज लिया गया। लिहाज़ा, सेक्स को लेकर लोगों में एक शर्म सी पसर गई थी, हर किसी के मन में या कहें कि पूरे समाज में। सेक्स करना ही नहीं, बल्कि सेक्स की चर्चा से भी संकोच करते थे।
सेक्स को चरित्र से जोड़ने का नतीजा यह हुआ कि सब चरित्रवान बने रहना चाहते हैं। इसलिए ऊपर से दिखाते हैं कि वे सेक्स नहीं करते, जबकि हक़ीक़त में सब लोग सेक्स करते हैं। हां, यह ध्यान रखते हैं कि उनके सेक्स करने के बारे में किसी को भनक न लगे। छुपाने की यही मानसिकता उन्हें मेडिकल स्टोर जाकर कंडोम या निरोध ख़रीदने से रोकती है। मेडिकल वाले से कंडोम मांगेंगे तो वह सोचेगा, “अरे यह आदमी सेक्स करने के लिए कंडोम मांग रहा है।” यही न… फिर हंस देगा। मेडिकल वाले की इसी हंसी का डर सेक्स करने से पहले निरोध नहीं ख़रीदने देता था। यह झिझक आज भी 25-30 या 40-50 साल पहले तो और भी अधिक थी।
लिहाज़ा, बाप-दादा ने सेक्स तो किए गए मज़े लेने के लिए, लेकिन उससे हमारे जैसे लोग पैदा होते रहे। पैदा होकर हम जीवन जीने के लिए देश की भीड़ में शामिल होते रहे। परिवार वाले पैदा हुए हम अवांछित लोगों को कमाने के लिए मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता भेजते रहे। इसी तरह थोक के भाव हमारे जैसे लोग पैदा होते रहे। हम देश के लिए भार और परिवार के लिए कमाने वाला बनते रहे। परिवार का पेट पालने के लिए शहर भेजे जाते रहे। इस देश का यही फलसफा है।
मैं जब से पैदा हुआ हूं, मुझे दिन में तीन-चार बार भूख लगती है। पेट खाने को कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। इस भूख पर भी मेरा कोई ज़ोर नहीं। जी हां, जैसे पैदा होने पर मेरा कोई ज़ोर नहीं था, वैसे ही भूख पर भी मेरा कोई ज़ोर नहीं है। लिहाज़ा, हर कुछ घंटे बाद पेट में भकोसने के लिए किसी खाने लायक वस्तु की तलाश करता रहता हूं। जहां भूख को शांत करने की संभावना दिखती है, वहीं क़तारबद्ध हो जाता हूं। कहीं कुछ मिल जाता, कहीं कुछ भी नहीं मिल पाता है। लेकिन उससे रुकना नहीं है। बस चलते ही रहना है।
20-25 दिनों से लगातार चल रहा हूं। कहां पहुंचा हूं, पता नहीं। शायद आधा से अधिक रास्ता पार कर गया हूं। नही, आधे से कम होगा अभी। रास्ते में लोग मिलते हैं, कहते हैं, “पैदल क्यों जा रहे हो, सरकार ने तुम लोगों के लिए ट्रेन शुरू कर दी है।” फिर कहते हैं, “टिकट की बुकिंग ऑनलाइन हो रही है।” मेरा ही नहीं मेरे साथ चल रहे सब लोगों का मोबाइल फोन कब का डिस्चार्ज हो चुका है। कुछ लोगों के पास स्मार्ट फोन है, पर उनका भी फोन बंद हो गया है। लिहाज़ा, मैं लोगों के साथ पैदल ही चला जा रहा हूं।
ख़ूब चलने पर भी देर रात तक 50-55 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पाता। इसलिए जहां छांव मिलता है, या जहां खाना बंट रहा होता है, वहां थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। पहले दिन तो उत्साह में दिन भर में 70 किलोमीटर चल लिया, लेकिन पैर ही नहीं शरीर टूटने लगा। दूसरे दिन बमुश्किल 15 किलोमीटर चल पाया। तीसरे 20 किलोमीटर। इसी तरह गति को बढ़ाता रहा। जैसे जीवन भर मजदूरी करने की आदत पड़ गई थी, अब पैदल चलने की आदत पड़ गई है।
रास्ते में ऐसे भी लोग मिलते हैं, जो कहते हैं, “पैदल मत जाओ। बस शुरू हो रही है। एक पोलिटिकल पार्टी ने एक हज़ार बस की व्यवस्था की है।“ थोड़ी उम्मीद बंधती है, कि शायद इन पांवों को और चलने की जहमत न उठानी पड़े। बसें आ जाएंगी तो थोड़ी राहत मिल जाएंगी। अपने गांव जल्दी पहुंच जाऊंगा।
लेकिन किसी दूसरे राहगीर ने बताया, “बस नहीं चलेगी। पार्टी ने एक हज़ार बस का वादा किया था, लेकिन नौ सौ पचास बसों की ही सूची दे सकी। इसलिए सरकार ने कहा कि चलेगी तो पूरे एक हज़ार बसें चलेगी। वरना एक भी नहीं चलेगी। पूरी योजना टांय-टांय फिस्स!”
सरकार को बसें चलाना चाहिए था, भले नौ सौ पचास बसें ही थीं। अरे सौ रही होतीं, तो भी चलाना चाहिए था। मैं सोचता हुआ चला जा रहा था।
फिर तीसरे राहगीर ने बताया, “सरकार ने बस चलाने का परमिसन नहीं दिया। बसों के पास परमिट नहीं था। इसलिए अब कोई बस नहीं चलेगी।”
मैंने उस राहगीर से पूछा, “बसों के पास परमिट नहीं था, डीज़ल तो था न भाई?”
राहगीर ने कहा, “हां, डीज़ल तो था, परतुं परमिट नहीं था।”
मैं मन ही मन बुदबुदाया, “इस संक्रमणकाल में, जब ज़िंदा रहने के लिए लोग सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे हैं, तब भी बसों के चलने के लिए डीज़ल से ज़्यादा परमिट क्यों ज़रूरी है भगवान? इस घनघोर संकट के समय भी सियासत!”
और आगे चलने पर किसी और राहगीर ने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा हुई है। मुझे पूरा यक़ीन था, वह 20 लाख करोड़ रुपए कम से कम किसी बस को चलाने के लिए नहीं हैं। इसलिए उस पैकेज से कोई उम्मीद पालना बेकार है।
बस मैं चलता रहा। मुझे पता है, गांव वाले भी गांव में घुसने नहीं देंगे। यह भी जानता था, कि क्वारंटीन कर देंगे, लेकिन खाना तो देंगे। खाने का नाम सुनकर शरीर में ऊर्जा आ गई और मैं तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। अपने गांव की ओर।
-हरिगोविंद विश्वकर्मा
इसे भी पढ़ें – क्या पुरुषों का वर्चस्व ख़त्म कर देगा कोरोना?
Share this content: