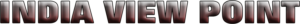हरिगोविंद विश्वकर्मा
कोई रो रहा है।
–कौन है? क्यों रो रहा है? किसके लिए रो रहा है? मैं ख़ुद से सवाल करता हूँ। अपने दिमाग़ पर ज़ोर डालता हूँ, -कौन हो सकता है? किसको पड़ी है, मुझ पर रोने की? किसको ज़रूरत है मेरी? एक नकारा, नाकाम, असफल और बेकार आदमी की।
कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। लेकिन असफल रहा। जीभ में हलका-सा कंपन होकर रह गया। आवाज़ निकली ही नहीं। अंदर ही घुट कर रह गई।
आवाज़ तो किसी स्त्री की लगती है। अभिलाषा की तरह लग रही है। हाँ, अभिलाषा ही है। मेरी धर्मपत्नी अभिलाषा। शायद रो रही है।
–लेकिन वह क्यों रो रही है? मैं मन ही मन सवाल करता हूँ, –वह मेरे लिए क्यों रोएगी? अब अचानक क्या हो गया, जो रो रही है? हैरान होता हूँ। मैं और थोड़ा सा खिन्न मन से सोचता हूँ। फिर दिमाग़ पर ज़ोर डालता हूँ और सोचता हूँ, –क्या वह मेरी हालत देखकर रो रही है? हाँ, शायद ऐसा ही है। शायद नहीं। नहीं-नहीं, ऐसा ही है। सौ फ़ीसदी ऐसा ही है। वह मुझे लाचार देखकर ही रो रही है।
फिर मेरा मन बदल जाता है।
कहना चाहता हूँ, –रोओ मत। अब कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे आख़िरी विदाई दो। वैसे भी अब मेरा चले जाना ही ठीक है। जिस आदमी का दुनिया में रहना, उसके दुनिया से चले जाने से ज़्यादा महँगा हो, उसका चले जाना ही ठीक। मैं बीमार आदमी। असाध्य रोग से पीड़ित। इसलिए मेरा चले जाना ही ठीक है। मेरा चिर-प्रस्थान करना कतई अनुचित नहीं होगा। वैसे, मैंने जीकर ही क्या किया? कौन-सा तीर मार लिया? सदैव अभावों से ग्रस्त रहा। हर समय पैसे-पैसे का मोहताज़। ज़िंदगी भर संघर्ष ही करता रहा। दो जून की रोटी जुटाने तक के लिए भी संघर्ष। कभी इधर से उधर, कभी इनके पास, कभी उनके पास… भटकता और भागता ही रहा। मैं जीवन के हर मोड़ पर लड़ता और हारता रहा। पराजय ही शायद मेरी नियति थी। साए की तरह ताउम्र साथ नहीं छोड़ी। मेरे दामन से चिपकी रही। जोंक की तरह मुझे चूसती रही। खोखला करती रही। मेरा आत्मबल, मेरा आत्मविश्वास, मेरा आत्मसम्मान सब कुछ हिलाती और छीनती रही। दोबारा बोलने की कोशिश असफल गई।
हालाँकि यह मेरे मरने की उम्र नहीं है। तीस साल की उम्र भी कहीं, मरने की उम्र होती है। परंतु मेरे साथ तो यही सच था। तभी तो मरणासन्न पड़ा हूँ, बिस्तर पर। कुछ-कुछ अर्धमूर्छित, अर्धचेतन अवस्था में। क़रीब-क़रीब सभी अंगों ने सक्रिय रूप से काम करना बंद कर दिया है। इंद्रियाँ भी शिथिल पड़ गई हैं। जो अंग थोड़े बहुत काम कर रहे हैं। वे कब थम जाएँगे, इसका कोई भरोसा नहीं। फिर भी सांस अभी तक चल रही है। ज़बान मारी गई है। बस, जीभ कुछ-कुछ फड़कती है। लेकिन बोलने में एकदम असमर्थ। बहुत ज़ोर देने पर गू-गू या हू-हू जैसी आवाज़ निकलती है।
रोने की फिर वही आवाज़ मेरे कान के परदे से टकराती है। संभवतः अभिलाषा को भी यक़ीन होने लगा है, कि अब वाक़ई मैं मर जाऊँगा। इसीलिए वह रो रही है। मैं थोड़ा कन्फ़्यूज़्ड होता हूँ। वह मेरे लिए रो रही है या अपने लिए? हाउसवाइफ़ है। हाउसवाइफ़ पराश्रित होती है। पति पर पूर्णतः निर्भर। अभिलाषा भी अपने रोज़मर्रा के ख़र्च के लिए पति यानी मुझ पर निर्भर है। हालाँकि बहुत दिन से वह मुझ पर निर्भर नहीं है। उसका ख़र्च मेरे परिवार वाले ही देख रहे हैं। फिर भी मैं उसका पति तो हूँ। हाउसवाइफ़ होने के नाते वह मुझ पर निर्भर तो है ही।
कुछ देर यूँ ही सोचता रहता हूँ। अचानक मन में सवाल फिर से उठता है कि वह मेरे जीवन के लिए रो रही है या अपने जीवन के लिए?
यहाँ एक नहीं, बल्कि दो जीवन हैं। एक, मेरा जीवन है, जो ख़त्म होने वाला है और दूसरा, अभिलाषा का जीवन है, जो मुझ पर निर्भर है और मेरे बाद भी रहने वाला है। यानी उसका जीवन भी मेरे जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा है। इसीलिए दुविधा में हूँ कि वह किस जीवन के लिए रो रही है। उस जीवन के लिए जो ख़त्म होने वाला है या उस जीवन के लिए जो रहने वाला है।
मेरी दुविधा बढ़ती जा रही है। मैं यह तय नहीं कर पा रहा हूँ कि वह मेरे लिए रो रही है या अपने लिए। शायद वह मेरे लिए ही रो रही है, क्योंकि अब मैं जीवन-यात्रा में आगे उसका साथ नहीं दे पाऊँगा। उसे मेरे जीवन की फिक्र है, आख़िर वह पत्नी है मेरी। मेरे बाद वह अनाथ हो जाएगी। उसका जीवन कष्टप्रद हो जाएगा। एकदम नारकीय। कहने का मतलब मेरे बहाने वह अपने लिए रो रही है कि मेरा जीवन के ख़त्म हो जाने पर उसका जीवन दिशाहीन हो जाएगा। परंतु मेरी दुविधा ख़त्म नहीं हुई। मुझे मृत्य-शैय्या पर देखकर उसे किस पर दया आ रही है? मेरे ऊपर या अपने ऊपर। पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या सच है। फिर वही उलझन, वह मेरे लिए रो रही है या अपने लिए।
जीवन के संक्षिप्त सफ़र के दौरान अक्सर मुझे लगा कि इस ज़माने में दो तरह के लोग हैं। पहले वे लोग, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। दूसरे वे लोग, जो अपने साथ-साथ दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, वे ज़्यादा सुखी रहते हैं। ज़्यादा ख़ुश रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, वे कुछ ज़्यादा ही दुखी रहते हैं। वे जीवन भर सुखी नहीं रह पाते हैं। कभी-कभी मुझे यह भी लगता है कि अधिकांश लोग केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं। यह समाज इसी तरह के लोगों से बना है, जो केवल अपने आपसे ही सरोकार रखते हैं।
–मैं क्या हूँ? अपने बारे में सोचने वाला या अपने साथ-साथ दूसरों के बारे में भी सोचने वाला? पता नहीं…
फिर मैं अपना आकलन करने लगता हूँ। अपने स्वभाव और अपने जीवन का विश्लेषण करने लगता हूँ। अपनी जीवन यात्रा पर सरसरी नज़र दौड़ाता हूँ। फिर कहता हूँ कि नहीं, मैं केवल अपने लिए ही नहीं जी सकता था। मैं केवल अपने बारे में नहीं सोच ही सकता था। मैं केवल अपने लिए जीने या सोचने वाला इंसान हीं नहीं रहा कभी। तो क्या मैं समाज के बाहर का आदमी हूँ? मैं समाज के अंदर का होऊं या बाहर का, लेकिन यह सौ फ़ीसदी सच है कि मैं इस समाज में मिसफिट हूँ, क्योंकि मैंने तो कभी केवल अपने बारे में नहीं सोचा। मैंने केवल अपने लिए कभी नहीं जिया।
मैं अपने आपसे दोबारा सवाल करता हूँ, क्यों नहीं जिया केवल अपने लिए मैं? क्यों नहीं सोचा मैंने केवल अपने बारे में? मैं क्यों नहीं हो सका सबके जैसा? उत्तर खोजने की कोशिश करता हूँ, परंतु कोई जवाब नहीं मिलता है। शायद मेरा स्वभाव ही ठीक नहीं था। तभी तो मैं केवल अपने लिए नहीं जी सका। वैसे मैं चाहता तो भी केवल अपने लिए जी भी नहीं सकता था। मैं आदमी ही अजीब किस्म का था। केवल अपने लिए ही जीना, मेरे लिए संभव ही नहीं था। यह मेरे डीएनए में ही नहीं था। आज के दौर के हिसाब से मेरा डीएनए ही ख़राब था। इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है। शायद मैं ख़ुद। मुझे प्रैक्टिकल होना चाहिए था, लेकिन मैं आदर्शवादी हो गया।
मुझे याद है। बचपन से ही मेरी माँ अक्सर मुझसे पाप और पुण्य की बात करती थी। दो बातें कहा करती थी। पहला- बेटा, झूठ कभी मत बोलना, झूठ बोलने से पाप लगता है। दूसरा, ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करना, ज़रूरतमंदों की मदद करने से पुण्य मिलता है। स्कूल गया तो वहाँ भी पाप और पुण्य का गणित समझाया गया। गीता उपदेश का हवाला देते हुए टीचर ने भी कहा, -झूठ बोलना पाप है और दूसरों की मदद करना पुण्य है। तब मुझे लगा कि माँ ने जो कहा था, वही टीचर भी बता रहा है। यानी माँ और टीचर सच बोल रहे हैं। दरअसल, माँ और टीचर ने जीवन के एक ही पक्ष की व्याख्या की थी। केवल यही बताया कि सच बोलना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि आज के दौर में न तो कोई सच बोलता और न ही कोई निःस्वार्थ दूसरों की मदद करता है।
दरअसल, हमारे समाज का स्वरूप ही ऐसा बन गया है कि यहाँ सच बोलना संभव ही नहीं। इस समाज में जो सच बोलता है, वह हाशिए पर चला जाता है। हँसी का पात्र बन जाता है। उसे देर-सबेर ख़ुदकुशी करनी पड़ती है। इस समाज में जिन्हें ज़रूरत है, वे कतार में ग़ैर-ज़रूरतमंदों द्वारा बहुत पीछे ढकेल दिए गए है। वे इतने दूर हैं कि मदद उन तक पहुंच ही नहीं सकती। जिन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, वही ज़रूरतमंद बन गए हैं। कहने का मतलब, मैं जीवन के इस दूसरे पक्ष से अनजान ही रह गया और माँ व टीचर की बातों को सच मान लिया। माँ की नसीहतों और टीचर की हिदायतों ने मेरा डीएनए ही बदल दिया। इनसे हासिल संस्कार कालांतर में मेरी कमज़ोरी बन गया। मैं दुनिया में अप्रासंगिक इंसान हो गया।
ज़रूरतमंदों की मदद करने की मेरी प्रवत्ति आगे चलकर मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी बन गई। मैं हर संकटग्रस्त आदमी की मदद के लिए आगे बढ़ जाता था। मैं किसी का दुख बिल्कुल देख नहीं पाता था। किसी को दुखी देखकर पता नहीं क्यों, मुझे बेचैनी-सी होने लगती थी। मुझे लगता था, मेरे साथ ही घट रहा है। दूसरों को दर्द में देखकर मुझे भी दर्द महसूस होने लगता था और मैं भी दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता था। इस बात को लेकर मैं व्याकुल रहता था कि क्या करूँ कि संकटग्रस्त आदमी का दर्द या दुख कम हो जाए। इस तरह हर दुखी या पीड़ित इंसान से अपने आप मेरा नाता जुड़ जाता था। मुझसे जो बन पड़ता था, वह करने लगता था। संभव होता था, तो उसकी मदद कर देता था। मदद करने की हैसियत न होने पर परेशान होता था। झुंझलाता था कि मैं इतनी हैसियत क्यों नहीं बना पाया कि हर ज़रूरतमंद की मदद कर सकूँ।
संभवतः माता लक्ष्मी देवी मुझ पर इसीलिए कभी भी मेहरबान नहीं हुईं, क्योंकि मैं उन्हें अपने पास सहेजने की बजाय ज़रूरतमंदों को दे देता था। ख़ुद लक्ष्मी भी जानती थीं कि वह मेरे पास जितना ज़्यादा आएँगी, मैं संकटग्रस्त लोगों को उतना ही दे दिया करूँगा, क्योंकि मेरी अपनी ज़रूरत तो सिर्फ़ दो जून की रोटी और दो जोड़ी कपड़े तक सीमित थी। इसके अलावा मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी। हालाँकि, कुछ लोग, नहीं-नहीं, ज़्यादातर लोग मेरे इस स्वभाव को मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी समझते थे। कई लोग तो मुझे निरा बेवकूफ़ ही समझते थे। यह भी मुमकिन है, कई लोगों ने इसका बेज़ा फायदा उठाया हो, या कई ग़ैर-ज़रूरतमंदों ने मुझसे मदद ले ली हो, लेकिन मुझे किसी से कोई भी शिकायत नहीं। कोई गिला-शिकावा या अफ़सोस नहीं। सबसे बड़ी बात यह थी कि जीवन में मेरा कोई बहुत ज़रूरी काम कभी नहीं रुका। हालाँकि मैं जीवन भर अभावग्रस्त ज़रूर रहा। मगर ऐन-केन-प्रकारेण काम चल ही जाता था।
बीमार होने पर मेरा इलाज हो रहा था, लेकिन बहुत महँगा था, इसलिए मैंने ही मना कर दिया। तब मैं इस तरह अर्धचेतन अवस्था में नहीं था। मैंने कहा, -मुझे घर ले चलिए और बिना इंजेक्शन के शांतिपूर्वक मरने दीजिए।
अभिलाषा के सिसकने की आवाज़ फिर कानों से टकराती है। फिर सोचने लगता हूँ, -नहीं-नहीं, अभिलाषा अपने लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए रो रही है। मुझ जैसे सक्रिय इंसान को इस तरह लाचार बिस्तर पर देखकर उसे दया आ रही है और रोना भी। फिर सोचने लगता हूँ। लेकिन मेरे लिए क्योंकर रोएगी वह? उसे जितना मैं जान पाया, उससे तो यही लगता है कि उसका स्वभाव बेशक बहुत अच्छा था, लेकिन उसने दूसरों के लिए परेशान होना या रोना सीखा ही नहीं था। दूसरों के लिए व्यथित होना उसके स्वभाव में नहीं था। शायद, शुरू से ही उसे अपने अलावा कभी किसी की चिंता नहीं रही। फिर भी लगता है, यह भी तो संभव है कि मैं उसके स्वभाव का आकलन करने में ग़लत रहा होऊँ, या हो सकता है, मैं उसके स्वभाव को समझ न पाया होऊँ। हाँ, यह भी संभव है कि मैं उसके साथ सालों-साल रहने के बावजूद उसे बिल्कुल नहीं समझ पाया होऊँ। वास्तव में इस समय वह मेरे लिए ही रो रही है। वह जैसी भी रही हो, उसे मेरे जीवन की फ़िक्र है। उसे मुझसे बिछड़ने की पीड़ा है।
वैसे, अभिलाषा का जो स्वभाव है, वह भले ही मेरे हिसाब से सही या अनुकूल न रहा हो, लेकिन उसके हिसाब से तो सही ही रहा है। वह ऐसे माहौल में ही बढ़ी-पली थी, जहाँ लोग केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। ऐसे लोग अपने बचपन से ही सेल्फ़-ओरिएंटेड हो जाते हैं। आज के दौर में इस तरह के लोगों को ही प्रैक्टिकल कहा जाता है। इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों के पास अपार दौलत होती है। उन्हें पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। उनके लिए पैसा पहले नंबर पर होता है और इंसान दूसरे नंबर पर। अभिलाषा भी शायद अपवाद नहीं थी। किसी की परवाह करना उसकी आदत में नहीं था। उसका जो व्यक्तित्व था, वह अलग क़िस्म का था। लेकिन उसके साथ भी न्याय नहीं हुआ। उसकी शादी किसी बहुत ही धनवान व्यक्ति से होनी चाहिए थी। तब उसके स्वभाव की जो ख़ासियत थी, वह संभव है उभरकर सामने आती। लेकिन वह मुझ जैसे स्वप्नजीवी पुरुष से ब्याह दी गई और मेरे साथ उसके अंदर की ख़ूबी ही दब गई या मर गई। मैंने उसे बेहतरीन ज़िंदगी नहीं दी, जो मुझे देना चाहिए था।
वस्तुतः मेरे पास बहुत पैसे नहीं थे। लिहाज़ा, हमारे बीच में वह रिश्ता नहीं बन पाया जो रिश्ता आमतौर पर दंपति के बीच में होना चाहिए। एक तरह से हमारे रिश्ते का आधार ही पैसा था। कुछ लोग धरती पर ऐसे भी होते हैं, जिन्हें केवल अपने आपसे प्यार होता है। हालाँकि असली परीक्षा की घड़ी में यूँ तो हर इंसान ख़ुदगर्ज निकलता है। लेकिन अभिलाषा में इसकी मात्रा मुझसे थोड़ी ज़्यादा थी। हमारे संबंधों का आधार पैसा नहीं होना चाहिए था। हमारे रिश्ते में प्यार का थोड़ा अंश होना ही चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी तो यह नौबत आई। इसमें अभिलाषा का दोष नहीं। दोष तो उस हालात का है जिसमें उसका पालन-पोषण हुआ था। इस तरह के हालात में पलने-बढ़ने वाले संकीर्ण सोच के हो ही जाते हैं। ये लोग प्रॉफ़िट-ओरिएंटेड होते हैं। संबंधों को भी हानि-लाभ के तराजू से तौलते हैं।
संभवतः अभिलाषा ने भी दांपत्य जीवन को हानि-लाभ के चश्मे से देखने की कोशिश की थी। वह ऐसा करने से ख़ुद को रोक भी तो नहीं सकती थी। उसकी सहेलियों और उसके आसपास की महिलाओं के पति बेशुमार दौलत कमा रहे थे। उसने वही उम्मीद मुझसे भी की थी। उसकी इस उम्मीद को अनुचित बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। आख़िरकार एक औरत के रूप में उसे भी सुख-सुविधा और ऐश्वर्य हासिल करने का उतना ही अधिकार था, जितने उसके आसपास की स्त्रियों को था।
दरअसल, हमारा समाज स्त्री-विरोधी समाज है। पुरुष अपनी सुविधा के लिए इसे पुरुष प्रधान समाज कहते हैं। पुरुष प्रधान समाज में पैसे कमाने की ज़िम्मेदारी पुरुष की होती है। जहाँ स्त्री भी कमाती है, उसे बोनस कह सकते हैं। इसलिए यहाँ अभिलाषा का रत्ती भर दोष नहीं। सारा दोष तो मेरा है। पता नहीं क्यों माँ और टीचर ने मुझे सतयुग का पाठ पढ़ा दिया। माँ को भी उसकी माँ ने यह पाठ पढ़ाया होगा। इसीलिए तो वह ख़ुद सदा अभावों में ग्रस्त रही, लेकिन ईमानदार रही। मुझे भी ईमानदारी का वही पाठ पढ़ाती रही। उसकी बात सुनकर मुझे भी लगता कि गीता, क़ुरआन या बाइबिल में लिखे उपदेशों पर चलना ही ठीक है। कल्याणकारी होता है। बहुत देर बाद पता चला कि इन धर्म ग्रंथों में लिखे उपदेशों पर जो भी चलेगा या जो भी नागरिक इनके मुताबिक जीवन जीने का प्रयास करेगा उसे, अतंतः असफलता ही हाथ लगेगी। वो असफलता उसे आत्महत्या का लिए मजबूर कर देगी। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपनी हत्या नहीं करनी पड़ी। उस कार्य को यह बीमारी कर रही है, जिसने मुझे ग्रसित कर रखा है।
इसमे दो राय नहीं कि अभिलाषा और मेरी सोच ही नहीं, बल्कि हमारे रहन-सहन भी बिल्कुल अलग-अलग थे। हमारी ज़रूरतों में भी भारी विरोधाभास था। जहाँ मेरी अपनी तो कोई ज़रूरत नहीं थी, वहीं उसके ज़रूरतों की बहुत लंबी फ़ेहरिस्त थी। हममें केवल एक बात कॉमन थी, वह था संगीत। उसमें भी उसे आज का तेज़ संगीत पसंद था तो मुझे पुराने दौर के दर्द उभारने वाले मधुर गीत पसंद थे। वैसे मैं भी पैसे को बुरा नहीं मानता था, क्योंकि आज के दौर में हर सुख-सुविधा जुटाने के लिए पैसे की ज़रूरत तो होती ही है। हाँ, पैसे को ही सब कुछ मैं नहीं मान सकता था। पैसा बेशक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पैसा मानव जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है?
कोई अचानक मेरे माथे पर हाथ रखता है। फिर नाड़ी पर हाथ रखता है। मैं उसके स्पर्श से पहचान नहीं पाया कि कौन है। सिर्फ़ महसूस भर कर सका। शायद वह डॉक्टर थे।
इसे भी पढ़ें – कहानी – हां वेरा तुम!
तक़रीबन आठ साल पहले मैंने इस शहर की धरती पर क़दम रखा। जल्द ही लगने लगा कि कर्म के लिए मैंने ग़लत स्थान का चयन कर लिया। कहाँ हरा-भरा और ख़ुशहाल मेरा गांव, और कहाँ कंक्रीट का बना यह शहर। एकदम संवेदनहीन। इमोशनलेस। यहाँ हर आदमी सुबह से शाम भागता ही रहता है। किसी को दूसरे से कोई मतलब नहीं। हर कोई अपनी ही दुनिया में मस्त। सबको केवल और केवल अपनी-अपनी चिंता रहती है। लोग बाग पास-पड़ोस में रहकर भी एक दूसरे से बिल्कुल अपरिचित ही रह जाते हैं। इंसानों की भीड़ होते हुए भी यहाँ अपना कोई नहीं होता था। मैं तो घबराकर ऐसे विचित्र शहर से पलायन करने वाला था कि नौकरी लग गई। वेतन भी ठीक-ठाक ही था।
अभी शहर से परिचित भी नहीं हुआ था कि एक दिन मेरे संरक्षक बड़े चाचाजी का आदेश सुनने को मिला, –नौकरी पक्की हो गई है। अपने पाँव पर खड़े हो गए हो। अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए।
मैं चुपचाप सुनता रहा। उन्होंने आगे कहा, –एक लड़की देखी है। ग्रेजुएट है… तुम्हारी जोड़ी ख़ूब जँचेगी।
मुझमें इनकार या प्रतिवाद करने की प्रवृत्ति ही नहीं थी। बचपन से मैंने केवल और केवल हाँ कहना ही सीखा था। ना कहना सीखने से अनजान रह गया। जिसने जो भी कहा, उसे ही सिरोधार्य कर लिया। कभी यह नहीं सोचा कि ग़लत है या सही। बस मान लेता था, हर किसी की बात। यहाँ बात जीवनसाथी की थी, फिर भी मौन ही रहा और मेरे मौन को बड़े चाचाजी ने मौन-स्वीकृति मान लिया।
हालाँकि मैं कहना चाहता था कि इतनी जल्दी भी क्या है शादी की। अभी थोड़ा सेटल्ड हो जाऊँ। कुछ पैसे कमा लूँ। शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाऊँ, तब कर दीजिएगा मेरी शादी। पर ज़बान ही नहीं खुली। बड़े चाचाजी ने रिश्ता स्वीकार कर लिया।
शादी के मंडप में ही मुझे लगा, बड़ी बेमेल शादी है। दोनों परिवारों का कोई मेल ही नहीं। अभिलाषा का परिवार महानगर की आधुनिक सोच वाला और मेरा परिवार गांव का परंपरावादी। दोनों परिवारों में भविष्य में शायद ही कोई समन्वय हो पाए। पता नहीं, अभिलाषा किस सोच की है। मेरे परिवार और मेरे जैसी है या फिर अपने परिवार और अपने जैसी। ज़ाहिर है वह अपने जैसी ही होगी। हमारी पटेगी कि नहीं? यह सवाल मेरे मन में कौंध रहा था जिसे लेकर मैं बहुत आशंकित था।
हमारे मिलन की पहली रात ही अभिलाषा ने बात-बात में पूछ लिया था, –सेलरी कितनी है?
पहले तो मुझे अटपटा लगा। मुझे उससे ऐसे प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। कुछ देर सोचता रहा। फिर धीरे से बोला, –अभी कनफर्म्ड हुआ हूँ। फिर भी कट-पिट कर जीवन-यापन भर के पैसे मिल जाते हैं। इससे परिवार का पेट भरने के बाद भी कुछ बचा लेता हूँ। मैंने बहुत ईमानदारी से बता दिया। हालाँकि बाद में लगा कि मुझे थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर बताना चाहिए था। वैसे भी मैं बढ़ा-चढ़ा कर बता भी नहीं सकता था, क्योंकि बढ़ा-चढ़ा कर बोलना, डींगें हाँकना या झूठ बोलना मैंने सीखा ही नहीं। यही मेरे व्यक्तित्व का सबसे कमज़ोर पक्ष बन गया।
–इतने से क्या होगा? सैलरी का अमाउंट सुनकर उसने बुरा-सा मुँह बनाया, –अपना घर कैसे बनाएँगे हम? सलोनी का हसबैंड दुबई में है। ख़ूब पैसे कमाता है। शादी के साल भर के अंदर टू बीएचके फ्लैट ले लिया। सुनंदा का पति भी सरकारी नौकरी में है, सेलरी के अलावा ऊपर से भी पैसे आते हैं। उसने एक फॉर्म हाउस ख़रीदा लिया है। मेरी दोनों सहेलियाँ रानी की तरह राज करती हैं। और मैं तो ग़रीब के साथ बाँध दी गई। पप्पा ने तो मुझे कहाँ फँसा दिया। अभिलाषा अपसेट थी और बड़बड़ाए जा रही थी। वह पूरी तरह अपसेट हो गई। उसे अपने पिता जी पर ग़ुस्सा आ रहा था। उसकी बात से मुझे यही लगा।
उसकी बात सुनकर मैं तो अवाक ही रह गया। कल्पनाओं की दुनिया से सीधे ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। मैंने फिल्मों में दिखाई जाने वाली पुराने ज़माने वाली सुहागरात की कल्पना की थी। जब शादी के बाद प्रथम मिलन के दृश्य में दूल्हा फूलों से सजे कमरे में प्रवेश करता है और बिस्तर पर घूँघट काढ़े बैठी दुल्हन किसी गुड़िया की तरह हया से झुक जाती है। फिर दूल्हा आहिस्ता-आहिस्ता उसका घूँघट उठाता है। स्त्री के घूँघट के पक्ष में मैं कभी नहीं रहा, लेकिन अपनी जीवन-संगिनी से सौम्य इंट्रोडक्शन की उम्मीद तो थी ही मुझे। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। नियति ने शायद मेरे साथ नहीं-नहीं, हम दोनों के साथ क्रूर मज़ाक़ कर दिया था। मेरी पत्नी अलग सोच वाली लड़की है। एकदम प्रैक्टिकल। तो क्या सचमुच उसके पिता ने उसे फँसा दिया या फिर मैं किसी ग़लत खूँटे से बाँध दिया गया? प्रथम मिलन की रात बेड के एक सिरे पर लेटा मैं यही सोचता रहा। उस रात हमारे बीच केवल इतनी ही बात हुई और थोड़ी देर में अभिलाषा बिंदास सो गई। लेकिन मेरे आँखों की तो नींद ही उड़ गई थी।
सब जगह से जबाव मिल गया है। हालाँकि मेरी बीमारी लाइलाज नहीं है। लेकिन है बड़ी महँगी। परिवार वालों की हैसियत से परे। घर के लोग यथाहैसियत इलाज करवा कर थक गए हैं। जब डॉक्टर ने बहुत महँगा इलाज रेफर किया तो सबके सब लोग लाचार हो गए। सभी लोग चाहते थे, मैं जीऊँ, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे। अब उनके हाथ में कुछ नहीं था। कहीं कुछ बेचने के लिए भी नहीं था कि बेचकर पैसे का जुगाड़ करते और मेरा इलाज करवाते। बड़े चाचाजी ने कई चैरिटी संस्थानों का चक्कर लगाया, कई लोगों के पास गए। पर कोई पहुँच न होने से कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। कहीं मदद मिल सकती थी लेकिन वह यह यक़ीन दिलाने में असमर्थ रहे कि वह वाक़ई में ज़रूरतमंद हैं।
सबसे अंत में डॉ. रवि टंडन ने कहा था, –बढ़िया इलाज न करवा पाने से अब ये टर्मिनल स्टेज में आ गए हैं। इनका बचना अब मुश्किल लग रहा है। आप लोग अब पैसे के लिए भी हाथ-पैर मत मारिए। इन्फेक्शन फेफड़े और लीवर तक पहुँच गया है, कुछ दिन में हार्ट और ब्रेन तक पहुँच जाएगा। कब दम तोड़ देंगे कुछ भरोसा नहीं। इसलिए अब दिल पर पत्थर रखकर इन्हें घर ही ले जाइए। कुछ नहीं हो सकता। जो हो सकता है, उसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है।
मतलब, आज मेरा जीवन पैसे का मोहताज़ है। पैसा नहीं है, तो इलाज नहीं होगा। इलाज नहीं होगा तो मरना होगा। बिल्कुल आम भारतीय नागरिक की तरह। मैं आम भारतीय नागरिक ही तो था।
–बड़े चाचाजी मुझे कमरे पर ले चलिए। मैंने भी कहा था।
बस क्या था, आख़िरकार मजबूरी में मुझे घर लाया गया और इस बिस्तर पर सुला दिया गया। अब सब लोग मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं भी मौत की ही राह देख रहा हूँ। कितनी विचित्र बात ही न। मौत आने वाली है, यह निश्चित है, बस किस समय आएगी यही तय नहीं है।
डॉ. टंडन की बात सुनकर मुझे डर नहीं लगा। मैं मौत से कभी डरा ही नहीं। उल्टे इस बार मौत के आगमन की ख़बर सुनकर ख़ुश ही हुआ। वैसे भी निरर्थक ज़िदगी जी रहा था। ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। चलो अच्छा हुआ कि जीवन आख़िरकार सिमट गया। जब तक जिया चैन की नींद ही मयस्सर नहीं हुई। अब चिर निद्रा में चैन से सोऊँगा।
लेकिन आज अभिलाषा का क्रंदन व्यथित कर रहा है। मेरे मरते ही वह विधवा हो जाएगी। युवा विधवा। मैंने युवा विधवाओं की हालत बहुत क़रीब से देखी है। किसी भी अनाथ विधवा का कोई नहीं होता। अपने भी पराए हो जाते हैं। अगर विधवा युवा है तो सबकी नज़र उसके जिस्म पर ही होती है। हर कोई उसे भोगने की वस्तु समझने लगता है। हर आदमी मदद करने की आड़ में उसे पाने की कोशिश करता है। लोग इसके लिए हमदर्द बनने का प्रपंच भी रचते हैं। शहीद होने वाले फौजियों की विधवाओं तक से यही व्यवहार होता है। इसीलिए ऐसे वहसी समाज में विधवा का जीवन बहुत कष्टप्रद हो जाता है। एकदम नारकीय। अभिलाषा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वह अनाथ नहीं होगी। उसके पिताजी सक्षम हैं। वह संभाल लेंगे। किसी अच्छे पुरुष से उसकी शादी करा देंगे। संभव है अपनी जायजाद का कुछ हिस्सा उसे दे दें। तब तो वह आर्थिक रूप से भी निश्चिंत हो जाएगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही हो। मेरी मौत से उसका जीवन सँवर जाए, मेरी मौत उसके लिए शुभ हो। उसके पिता ने मेरे साथ उसकी शादी करके जो ग़लती की है, उसका भूल-सुधार हो जाए।
दरअसल, अभिलाषा का मेरे साथ विवाह एक तरह से एक हादसे जैसा था। आजकल परंपरागत शादियाँ यानी अरेंज मैरिज हादसे जैसी ही हो गई हैं। हादसे में संयोग ठीक रहा तो वर और कन्या बाल-बाल बच जाएँगे। यानी अगर अपने जैसा स्वभाव वाला जीवन साथी मिल जाता है तो ज़िंदगी फूलों की सेज बन जाती है, लेकिन अगर हादसे में संयोग नहीं ठीक नहीं रहा तो नवदंपति का जीवन नारकीय हो जाता है। अरेंज मैरिज के नाम पर अगर दो विपरीत विचार एवं पसंद वाले इंसानों को एक खूंटे से बांध दिया गया, तो वे न जी पाते हैं न ही मर पाते हैं। जहाँ-जहाँ भी ऐसा होता है, वहाँ-वहाँ पति और पत्नी दोनों का जीवन ही कष्टप्रद हो जाता है। इसलिए, अरेंज मैरिज जैसी सदियों पुरानी प्रथा का विकल्प तलाशने की ज़रूरत है, ताकि लोग जीवन को जीएँ, न कि उसे झेलें। शादी या दूसरे संबंधों में भूल-सुधार का विकल्प होना चाहिए।
पता नहीं क्यों, मैं अभिलाषा का क्रंदन सह नहीं पा रहा हूँ। मुझे वही पीड़ा हो रही है, जो किसी को दुख में देख कर होती रही है। मेरी व्यथा अभिलाषा के स्वभाव के कारण नहीं है। मुझसे उसके अंदर की स्त्री को रोते हुए नहीं देखा जा रहा है। आख़िर उसके अंदर की स्त्री मेरी पत्नी है। वह मेरी ज़िम्मेदारी है। मुझे याद है, सात फेरे लेते समय मैंने उसे सुखमय जीवन देने का वादा किया था। वह वादा तो मैं निभा ही नहीं सका। मैं ही असफल साबित हुआ। मेरी असफलता या मेरे स्वभाव की क़ीमत वह क्यों चुकाए। मैं उससे उस चीज़ की उम्मीद करता रहा, जो उसके स्वभाव में ही नहीं था। इसमें उसका क्या दोष? एक आम लड़की की तरह उसका अपने आसपास की लड़कियों से अपनी तुलना करना तनिक भी ग़लत नहीं था। यहाँ सारी ग़लती मेरी ही है। ग़लती पूरी तरह मेरी भी नहीं है, ग़लती तो अरेंज मैरिज की उस परंपरा की है, जिसके चलते हम दो अलग-अलग विचार के लोगों को पति-पत्नी बना दिया गया।
इसीलिए अचानक अब यह ख़याल आ रहा है कि अभी मैं न मरूँ। लेकिन क्या यह मेरे वश में है? नहीं, बिलकुल नहीं। जिस तरह पैदा होना, मेरे वश में नहीं था, उसी तरह अब मरना भी मेरे वश में नहीं है। या कहूँ कि मेरे जीवन पर मेरा कभी वश ही नहीं रहा, तो अधिक उपयुक्त होगा। मेरे साथ हरदम वही हुआ, जिस पर मेरा कोई वश नहीं था। इसीलिए हर घटना को अपनी नियति समझ कर स्वीकार करता रहा। जीवन भर दूसरों के ही फ़ैसले पर जिया। ख़ुद कभी कोई फ़ैसला नहीं ले सका। कभी-कभी सोचता हूँ, ऐसा क्यों होता रहा। मेरा व्यक्तित्व इतना कमज़ोर क्यों रहा। कोई जवाब नहीं मिलता।
ओह, ज़ोर से प्यास लगी है। हलक सूख रहा है। बग़ल में पानी रखा हुआ है। लेकिन कोई पिला नहीं रहा है। किसी को पता ही नहीं, कि मैं प्यासा हूँ और मेरा हलक सूख रहा है। मैं पानी के लिए तड़प रहा हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति भी नहीं कि पानी के पात्र से पानी ले सकूँ। बोलने में एकदम असमर्थ हूँ, सो पानी पिलाने के लिए किसी से आग्रह भी नहीं कर सकता। हाथ भी नहीं हिल रहा है कि कोई इशारा ही कर सकूँ कि थोड़ा पानी पिला दो। शायद अंतिम समय में लोगों को पानी पिलाने की परंपरा इसीलिए रखी गई है कि मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति, जो बोल पाने में असमर्थ है, का प्यास के चलते प्राण ना निकले। देखिए न, मेरे साथ जीवन की आख़िरी बेला में भी वही हो रहा हैं जो जीवन भर होता आया।
जीवन भर मैं तड़पता ही तो रहा। जो चाहा उसे पा ही नहीं सका। कोई भी चीज़ पहुँच से बाहर नहीं थी। लेकिन मेरे हाथ ही आगे नहीं बढ़े। न मालूम किस संकोच ने ज़बान पर ताला लगाए रखा। किसी मृग की तरह, मरीचिका की तलाश में इधर से उधर भागता रहा। दर-दर भटकता रहा। ठोंकरें खाता रहा।
उपन्यास पढ़ने की आदत बचपन से हो गई थी। प्रेम कहानी पर आधारित उपन्यासों को ख़ूब पढ़ता था। प्रेम कहानी लिखने वाले कथाकार मेरे प्रिय होते थे। हर उपन्यास एक ही सीटिंग में ख़त्म कर देता था। प्रेम कथा प्रधान उपन्यासों को तो कई-कई बार पढ़ जाता था। उपन्यास पढ़ते-पढ़ते कब प्यार पाने की हसरत मन में पलने लगी, पता ही न चला। कल्पनाओं में मुहब्बत करने लगा। कल्पनाओं में नायिका का सृजन करने लगा और उस पर ही प्यार न्योछावर करने लगा। बड़ी इच्छा थी कि मेरी कल्पनाएँ हक़ीक़त में तब्दील हों। सो, कॉलेज के दौर से बड़ी हसरत थी कोई लड़की मुझे प्यार करे। कोई मेरी फिक्र करे। मेरी केयर करे। किसी से अपनत्व के दो बोल सुनने को मिलें। कोई पूछे, कैसे हो? खाना खाए या नहीं? या पूछे कि क्यों खोए-खोए से रहते हो? एकदम अगल-थलग क्यों है तुम्हारा यह जीवन? आख़िर कौन सा काँटा है जो तुम्हारे हृदय में चुभता रहता है? तुम्हें जीवन में किसकी तलाश है? लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी से प्यार का एक लफ़्ज़ भी सुनने को नहीं मिला। ईश्वर ने मुझे प्रेम करना तो सिखा दिया लेकिन मेरे हिस्से प्रेम लिखना ही भूल गया। प्यार तो दूर प्यार का एक क़तरा भी मयस्सर नहीं हुआ।
अभिलाषा के स्वभाव में भी प्यार और केयर करने वाला पक्ष ही नदारत था। कभी-कभी मैं बड़ा हैरान होता था, उसके स्वभाव पर। सोचता कि कैसी स्त्री है, कभी रोमांटिक नहीं होती है। कभी प्यार भरी बातें नहीं करती है। पता नहीं क्यों वह हमेशा मुझसे चिढ़ी रहती थी या ग़ुस्से में रहती थी। इस वजह से मैं अकेला ही रह गया। निपट अकेला। दुनिया की भीड़ में एकदम तन्हा। नदी के किनारे रहकर भी प्यासा। सेक्स की इच्छा प्रबल होने पर बाथरूम चला जाता था।
तभी तो स्नेह का केवल एक अल्फाज़ भर बोलने वाली स्त्री की ओर बरबस मुड़ जाता था। जैसे पथिक कुएँ की ओर। प्यार के अल्फाज़ को सही मान लेता था। भावनात्मक रिश्ता बन जाता था। बाद में पता चलता था, सब मेरा भर्म था, पागलपन था। जो कुछ भी था, सिर्फ़ मेरी तरफ़ से था। रिश्ता एकतरफ़ा था। अमुक स्त्री को मुझसे कोई काम था। वह काम निकाल रही थी। मैं फटाक से धरातल पर आ गिरता था।
इसे भी पढ़ें – क्या पुरुषों का वर्चस्व ख़त्म कर देगा कोरोना?
आँखों के कोने से आँसू गिर रहे हैं। शायद मेरी आँखें भी मेरी इस लाचारी पर रूदन कर रही हैं। ज़बान आँखों का साथ नहीं दे पा रही है। तभी तो केवल आँसू गिर रहे हैं, आवाज़ नहीं निकल रही है। इसलिए रो नहीं पा रहा हूँ। हालाँकि जीवन की इस अंतिम बेला में जी भर कर रो लेना चाहता हूँ। दिल के सारे दर्द को, सारी पीड़ा और टीस को आँसुओं के साथ बहा देना चाहता हूँ। ताकि हल्का होकर महाप्रयाण कर सकूँ, लेकिन यहाँ भी वही लाचारी है। आँसुओं को ज़बान का साथ नहीं मिल पा रहा है।
कोई आँसू पोछ रहा है। सिसक भी रहा है। यह थकी हुई सिसकी अभिलाषा की ही है। अब वह भी रो-रोकर थक गई है। इसलिए केवल सिसक रही है। जैसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी ‘मंत्र’ में डॉ. चड्ढा के बेटे कैलाश के लिए उसकी प्रेयसी मृणालिनी रोते-रोते थक जाती है और अंत में निर्जीव सी दिखने वाली देह के पास बैठी सिसकती है और सुबह होने का इंतज़ार करती है। ताकि कैलाश का अंतिम संस्कार किया जा सके। मेरे घर वालों, ख़ासकर अभिलाषा, की भी वही स्थिति है। बस अंतर इतना है कि प्रेमचंद की कहानी में फ़रिश्ता बनकर भगत आ गया था और कैलाश को मौत के मुँह से खींच लिया था। लेकिन मेरे पास कोई भगत नहीं आने वाला है। अब इस दुनिया में भगत हैं ही नहीं। या कहें आजकल सारे भगत मर गए। नहीं-नही, आधुनिकता यानी विकास ने सारे भगतों की हत्या कर दी। इस समाज में कोई भगत ही नहीं बचा। चुन-चुन कर भगत जैसे सारे प्राणी मार दिए गए। यह दुनिया भगतरहित हो गई। आज़ादी के बाद हमने ऐसा समाज बना लिया कि अब हर जगह भगत की जगह चड्ढा ही चड्ढा हैं। उनके लिए मरीज़ से ज़्यादा ज़रूरी गोल्फ का खेल है। या फिर पेशेंट उनको क्लाइंट जैसा दिखता है, जो मुनाफ़ा देता है। पंच-सितारा अस्पतालों में तो मरीज़ की जगह क्लाइंट शब्द लिखा जाने लगा है।
मैं जिस कंपनी में नौकरी करता था, वहाँ अच्छी पोज़िशन में था। सेलरी भी अच्छी थी। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। लेकिन मेरे स्वभाव ने सब गुड़-गोबर कर दिया। निचले तबक़े के लोगों से लगाव बचपन से ही था। कार्यस्थल पर भी निचले तबके के कर्मचारियों से हमदर्दी थी। आख़िर उनकी जेनुइन प्रॉब्लम से कैसे मुँह मोड़ लेता। लिहाज़ा, विभाग में ऊपर गोपनीय रिपोर्ट चली गई कि मैं निचले तबक़े के कर्मचारियों का पक्ष लेता हूँ। उनके हित की बातें करता हूँ। मेरे ऊपर संस्थान के विरोध में काम करने का आरोप लग गया। जाँच हुई। पूछा गया कि कर्मचारियों से हमदर्दी है या नहीं। मैंने कह दिया, वे भी इंसान हैं। उनकी समस्याओं से मैं मुँह नहीं मोड़ सकता। बस क्या, मुझसे मेरा इस्तीफ़ा ले लिया गया। नौकरी से हटाए जाने के बाद सड़क पर आ गया। अचानक से उस समय समाज सेवा की सनक सिर पर सवार हो गई थी।
स्कूल के दिनों से ही लेखन और ज़रूरतमंदों की मदद करने का शौक़ था। यहाँ शहर में कई एनजीओ से अच्छे संबंध बन गए थे। उनके लिए काम करने लगा। उनके एक प्रोग्राम में शहर के बड़े संपादक से मुलाकात हो गई। वह मुझसे ख़ासे इंप्रेस्ड हुए। उन्होंने अपने लिए लिखने को कहा और मैं उनके अख़बार में लेख और रिपोर्ट लिखने लगा। फिर शहर के कई दूसरे अख़बारों से बतौर स्वतंत्र लेखक जुड़ गया। मेरा लेखन उत्तरोत्तर निखरता गया। क़लम की धार पैनी होती गई।
इसे भी पढ़ें – कहानी – डू यू लव मी?
इस दौरान उस एनजीओ से भी जुड़ा रहा। प्रचार सामग्रियाँ तैयार कर देता था। बाद में एक दूसरे एनजीओ की मैगज़ीन से बतौर संपादक फुलटाइम जुड़ गया। वहाँ बाहर लिखने की भी आज़ादी थी। घर में ठीक-ठाक पैसे आने लगे। मुझे लगा कि अब सही ट्रैक पर आ गया हूँ। समाज के शोषित तबक़े के लिए कुछ कर सकता हूँ। मेरे ऊपर समाज को सुधारने का भूत अब भी उसी तरह सवार था।
काश, उसी समय पता चल गया होता कि समाज या दुनिया में जो हो रहा है, वह होता रहेगा। मैं ही नहीं, बल्कि हर समाज सुधारक कुत्ते की तरह भौंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रॉ मैटेरियल ही सही नहीं है। सारे उत्पाद उसी से बनते हैं। जब रॉ मैटेरियल ही ठीक नहीं तो उत्पाद कैसे ठीक हो सकते हैं। इसीलिए चाहे कार्यपालिका हो या विधायिका या फिर न्यायपालिका हो, सब जगह डिफेक्टेड लोग हैं। केवल इन तीनों जगह नहीं, बल्कि बाक़ी जगह, चाहे वह पुलिस हो, मीडिया हो या दूसरे संस्थान, केवल डिफेक्टेड लोग भरे पड़े हैं। इसलिए पूरा सिस्टम ही डिफेक्टेड है। इस सिस्टम को दुरुस्त करना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि टेक्निशियन ख़ुद डिफेक्टेड है।
काम करते-करते एनजीओ से मेरा भावनात्मक रिश्ता बन गया था। इसलिए एक दिन जब अचानक बॉस ने कहा कि आप अपना फूल एंड फाइनल हिसाब ले लीजिए तो सदमें में आ गया। उन्होंने जो तर्क दिए, सब कमज़ोर थे। मैं एनजीओ की इमारत के बाहर आया और फूट-फूटकर रोया। मुझे लगा बुराइयों और असामाजिक तत्वों से लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहने वाला मेरे अंदर का व्यक्ति ख़ुद बहुत लाचार और शोषित है। मुझसे तो मेरा मकसद ही छिन गया। बाद में पता चला कि एनजीओ की मैगज़ीन में प्रकाशित मेरे किसी लेख से बॉस की धार्मिक भावनाएँ आहत हो गई थीं। लिबरल और सेक्यूलर का लाबादा ओढ़े वह बेहद कट्टर इंसान थे। बाद में और खुलासा हुआ कि वह बेईमान और धोखेबाज़ भी थे। फंड की हेराफेरी में जेल भेज दिए गए फिर सज़ा हो गई। कालांतर में मैंने देखा कि जितने लोग भी एनजीओ चलाते हैं, सबके सब पैसे बनाने के जादूगर होते हैं, समाज सेवा की आड़ में पैसे बनाते हैं।
एनजीओ मेरे लिए मेरा दूसरा घर था। मेरा मकसद था। लिहाज़ा, वहाँ आना-जाना बंद होने से मैं बहुत अंदर तक आहत हुआ। मुझे सदमा सा लगा। इस सदमे ने मुझे बीमार कर दिया। लेखन से भी मन उचट गया। मैं समझ गया कि कम से कम नौकरी करने वाला कोई व्यक्ति कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता। मतलब, सेलरीड पत्रकार चाहे वो छोटा सा संवाददाता हो अथवा सर्वशक्तिमान संपादक, कोई भी निष्पक्ष नहीं हो सकता है। लोग निष्पक्ष और ईमानदार होने का भ्रम पाल सकते हैं, लेकिन हो नहीं सकते। जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें कहीं न कहीं, किसी न किसी स्तर पर किसी न किसी की चाटुकारिता या चमचागिरी करनी ही पड़ती है। चमचागिरी या चाटुकारिता के क़्वांटम का स्तर अलग-अलग हो सकता है, लेकिन नौकरी के साथ वह अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। दरअसल, यहाँ बुनियाद में ही गड़बड़ी है। यह लेखन से ठीक भी नहीं होने वाला है। इसके लिए क्रांति की ज़रूरत है, जो अब नामुमकिन सी लगती है।
अब मैं ख़ाली था। फिर कुंठित होने लगा। धीरे-धीरे टूटने लगा। अंत में बुरी तरह टूट गया। मेरी हालत उस प्रेमी की तरह हो गई जो किसी बेवफ़ा से ताउम्र मोहब्बत का भ्रम पाले रहा। अंत में पता चलता है कि वह जिससे बेपनाह मुहब्बत करता रहा, वह उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। पता नहीं कौन सी ग़ुमनाम बीमारी ने मुझे डँस लिया। रोग बढ़ता रहा, धीरे-धीरे मेरे पूरे जिस्म को अपनी आगोश में ले लिया। मैंने यथाशक्ति इलाज करवाया। इलाज के दौरान मैंने पाया कि हर डॉक्टर मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मेरा जिस्म, जिस्म न होकर प्रयोगशाला हो गया है। इन प्रयोगों के चलते मेरा जिस्म जर्जर होता चला गया। डॉक्टर जाँच करवाते थे, फिर टेबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन देते थे। इतनी दवाइयाँ खाया कि धीरे-धीरे मेरा शरीर मेडिकल स्टोर में तब्दील हो गया। अंत में मुझे लाइलाज घोषित कर दिया गया, क्योंकि इलाज बहुत महँगा था। तो मैंने ही दवा खाने से इनकार कर दिया।
–क्या ज़िंदगी का कोई विकल्प होता है? एक बार दफ़्तर में एक सहकर्मी से मैंने पूछ लिया था।
–क्या कह रहे हैं आप सर? ज़िंदगी का विकल्प? वह चौंक पड़ी थी मेरा सवाल सुनकर। नहीं-नहीं उसकी आँखें फटी रह गई थीं। वह सिहर-सी उठी थी। उसके ज़बान से निकला था।
–हाँ। ज़िंदगी का विकल्प।
–तो क्या आप।
–हाँ, मैं ऊब चुका हूँ, इस जीवन से। इसलिए विकल्प तलाश रहा हूँ। तुम्हीं कोई रास्ता सुझाओ। कोई विकल्प बताओ।
–ज़िंदगी के प्रति इतनी घनघोर निराशा अब तक मैंने किसी में नहीं देखा। जितनी आपमें देख रही हूँ। फिर उसने कहा था। मुझे आप मृत नज़र आ रहे हैं।
आज लग रहा है, सही पहचाना था उसने। यक़ीनन कल्पनावादी से मैं निराशावादी हो गया था।
सहसा मेरी कलाई पर दवाब बढ़ता है। कोई मेरी नाड़ी चेक कर रहा है। शायद कोई डॉक्टर है। मेरी पुतलियाँ उठाकर आँखों का भी मुआयना कर रहा है।
–फ़िलहाल नाड़ी बहुत मंद चल रही है। पर किसी भी वक़्त रुक सकती है। यह डॉक्टर का निष्कर्ष था। उसकी उंगलियाँ मेरी नाड़ी पर ही थीं।
–क्या नाड़ी भर चलने से किसी को ज़िंदा कहा जा सकता है? मैंने फिर सोचने लगा, –क्यों नाड़ी के कंपन को जीवन का पर्याय मानते हैं लोग? जीवन के लिए नाड़ी का चलना क्यों ज़रूरी है? क्यों जीवन का बाक़ी प्राथमिकताएँ गौण होती हैं।
उफ्, फिर उन्हीं सवालों के मकड़जाल में उलझता जा रहा हूँ, जिनमें जीवन भर उलझा रहा। और, कभी उत्तर नहीं खोज पाया। उत्तर की ही तलाश में भटकता रहा दूर-दूर तक, बहुत दूर तक मगर उत्तर का कोई नामोनिशान तक नज़र नहीं आया। और ज़िंदगी का साँझ बेला में भी उत्तर से वहीं दूरी। ओह, कैसा जीवन जिया मैंने। जब-जब ज़िंदगी का मूल्यांकन किया सिफ़र ही हाथ लगा। आज भी सफलता का परिणाम शून्य ही है। नहीं-नहीं, शून्य भी नहीं। शून्य से भी नीचे। मेरी सफलता का योग ऋणात्मक है।
अचानक नाड़ी पर हाथ रखे डॉक्टर ने कुछ कहा। उनकी बात सुनते ही आसपास क्रंदन बढ़ गया। मगर सामूहिक रूदन अब कान के परदे को कंपित नहीं कर रहा था। निद्रा चिरनिद्रा में तब्दील हो रही थी। कहना चाहा, हे राम। मैंने अपनी तरफ़ से तो बुदबुदाने की पूरी कोशिश की लेकिन इस बार जीभ में कंपन भी नहीं हुई। मुझे हे राम कहना भी मयस्सर नहीं हुआ।
शायद जीवन की आख़िरी डोर भी टूट गई। जिस्म भी पार्थिव हो चुका था।
इसे भी पढ़ें – कहानी – एक बिगड़ी हुई लड़की
Share this content: