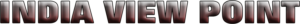सरोज कुमार
लोगों की भागीदारी से बनने और चलने वाला तंत्र लोकतंत्र कहलाता है। तंत्र पर चंद लोगों का वर्चस्व कायम हो जाए, फिर तंत्र चंद लोगों के हित में चलने, काम करने लगे, तब इसे क्या कहेंगे? वर्चस्व का अंकुर तो कामना से ही फूटता है। कामना ही बलवती होकर लोभ का रूप लेती है। यानी यह लोभ-तंत्र है! लोकतंत्र में हित सधता है, मगर सबका हित, यानी जनहित। जबकि लोभ-तंत्र में चंद लोगों का हित सधता है, और बाकी हित के साधन बन जाते हैं। यानी निहति स्वार्थ। हमारे देश की परिस्थिति आज क्या इससे कुछ अलग है? आत्मा कहती है हां, मगर अनुभव कहता है नहीं! यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोक-तंत्र लोभ-तंत्र में बदल चुका है!
लोभ-तंत्र राज-तंत्र की सीढ़ी है तो राज-तंत्र तानाशाही का सिंहद्वार, और तानाशाही फासीवाद का मुकम्मल चेहरा। और जो चेहरा आज हर जगह चमक रहा है, ध्यान से देखिए, उसमें यही फासीवाद दिखाई देगा। बाकी सभी चेहरे इस एक चेहरे को चमकाने का साधन बन चले हैं। यह एक डरावना दृश्य है। ये सबकुछ उस धरती पर हो रहा है जहां से राज-तंत्र और तानाशाही को एक बार नहीं बार-बार जड़ से उखाड़ फेंका गया है। और यह पुरुषार्थ यहीं के पुरुषों ने, महिलाओं ने किया है। राजाओं-महाराजाओं के जमाने में भी लोक ने उसी तंत्र को पूजा जिसका बरतने का तरीका लोक केंद्रित, लोकतांत्रिक था। ऐसे कई उदाहरण हमारे शास्त्रों, इतिहास की किताबों में उपस्थित हैं। राजतंत्र को, तानाशाही को, उस युग में भी यहां के लोक ने रत्तीभर नहीं संेटा। यानी लोक-तंत्र यहां के लिए पर-लोक की कोई वस्तु नहीं है। यह सभी के धमनी-तंत्र में प्रवाहित होने वाली वह रक्त संचेतना है, जिसके दम पर ही धरती का यह भू-भाग अबतक ’वसुधैव कुटुंबकम’ का दम भरता रहा है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता रहा है। ऐसे लोकतंत्र की उस संचेतना को आखिर अब क्या हो गया? ऐसा क्या कुछ घट गया कि सभी ने बत्तियां बुझा लीं, दरवाजे-खिड़कियां बंद कर लीं, और स्वयं को अपने ही घरों में कैद कर लिए!
लोक-मर्दन की मुनादी हो रही है! फासीवाद चढ़ा आ रहा है! फिर भी यह चुप्पी! सियापा! आखिर क्यों? हम इतने भयभीत क्यों हैं! लोक में यह चुप्पी लोभ के कारण ही तो नहीं? इसमें संशय नहीं। क्योंकि ये ईसा का दयाभाव तो नहीं है। चुप्पी यानी भय, लोभ का ही स्थायी भाव है। तो क्या हम लोभी हो गए हैं? लोकार्थ के साधक के बदले स्वार्थ के भोगी बन गए हैं? यदि ऐसा है तो फिर लोकतंत्र कहां बचा! गीता में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर मनुष्य के षड्रिपु बताए गए हैं। षड्रिपु यानी छह शत्रु। मगर ये सभी एक ही धातु के हैं। यानी सबकी आत्मा एक है। शत्रु का क्रियारूप शत्रुता है, और शत्रुता सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए होती है। शत्रुता कभी न्यायसंगत नहीं होती। और अन्याय का प्रतिकार न करना उससे बड़ा अन्याय होता है। अन्याय यानी पाप। गीता यही कहती है। फिर तो लोभ के वशीभूत होकर लोक का यह आत्मसमर्पण दोतरफा पाप हुआ, सबसे बड़ा पाप! महात्मा गांधी ने भी कहा था, ’’अन्याय करना जितना बड़ा जुर्म है, अन्याय का प्रतिकार न करना उससे बड़ा जुर्म है।’’ तो क्या हम जुर्म के जातक बन गए हैं! बापू ने यह भी कहा था कि अन्याय का मुकाबला सिर्फ सत्य के हथियार से ही किया जा सकता है। क्योंकि अन्याय से लड़ने की पहली शर्त निर्भयता है। और निर्भयता का स्रोत सत्य है। यानी हम डरे हुए लोग सत्यहीन भी हो गए हैं! यह तो बड़ी विडंबना है भाई!
सिकंदर आया तब यहां लोकतंत्र था। लोक की ताकत ने ही उसे यहां से खदेड़ा था। मुगल आए तब भी लोकतंत्र था। अंग्रेजों के समय भी यहां लोकतंत्र जीवंत था। ब्रिटिश इंडिया का पहला कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मैटकॉफ अपने चर्चित मिनट में लिखता है, ’’भारत के हरेक गांव अपने आप में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हैं। ये अपनी सभी जरूरतें स्थानीय स्तर पर ही पूरी कर लेते हैं। इन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। ये गांव अपने आप में अलग-अलग गणराज्य की तरह हैं। यही वजह है कि यहां बड़े-बड़े राजे-महराजे आए और चले गए, मगर ये गांव जस के तस बने रहे। मेरी इच्छा है इस व्यवस्था के साथ छेड़-छाड़ न किया जाए।’’ ब्रिटिश महाराजा को 1836 में भेजे गए इस मिनट से स्पष्ट है कि यहां कोई तो ऐसी व्यवस्था थी, जिसके दम पर गांव स्वतंत्र, आत्मनिर्भर गणराज्य की तरह मजबूत खड़े थे। हालांकि अंग्रेज तो यहां छेड़छाड़ के लिए ही आए थे। उन्होंने व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ ही नहीं किया, इसे तोड़ने-मरोड़ने-निचोड़ने की भी कोशिश की। कुछ टूट फूट हुई भी। मगर लोकतंत्र फिर भी अटूट बना रहा। धमनियों में संचरित होता रहा।
महात्मा गांधी ने लोकतंत्र की इस बुनियाद को पहचाना था। उन्होंने तभी ग्रामस्वराज की परिकल्पना पेश की थी, उसे जमीन पर उतारने की पुरजोर कोशिश भी की। उन्हें पता था कि ग्रामस्वराज के बिना लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, टिक नहीं पाएगा। बापू ने पहली जनवरी, 1948 को हरिजनसेवक में लिखा था, ’’सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे हुए 20 आदमियों से नहीं चल सकता। उसे हर गांव के लोगों को नीचे से चलाना होगा।’’ बापू ने लोकतंत्र को लेकर ये बात कोई एक-दो बार नहीं, बार-बार कही थी। लेकिन आज तो गांव अंतिम सांसें गिन रहे हैं। कैसी-कैसी तरकीब से गांवों को तोड़ा गया है, तोड़ा जा रहा है। जो काम आक्रांता नहीं कर पाए, उसे हमारे अपने चुने हुए भ्राताओं ने कर दिखाया है। आक्रांताओं को शायद हमारी उस धमनी का पता नहीं था, जहां लोकतंत्र संचरित होता था। अपने भ्राता तो लोकतंत्र की नस नस जानते हैं। उनके लिए यह काम आसान हो गया।
यहां हम गिनाना नहीं चाहते कि क्या कुछ, और कितना कुछ हो चुका है। अभी क्या कुछ और कितना कुछ हो रहा है। सबकुछ सभी के सामने है। जो हो रहा है दिन के उजाले में। जो होने वाला है, उसकी धमक भी साफ सुनाई दे रही है। दरअसल, किसी तंत्र को खत्म करने के पीछे खास उद्देश्य होता है, किसी दूसरे तंत्र की स्थापना। आज लोकतंत्र के स्थान पर जिस तंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य साफ दिखाई दे रहा है, उसका नाम फासीवाद है। वही फासीवाद जिसे उसकी जन्मस्थली पर ही आज पांव रखने की जगह नहीं बची है। वहां के लोक ने यूरोप से उसे कब का खदेड़ दिया है। मगर मुसोलिनी के नकली वारिश उसे आज राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर, महावीर, नानक और गांधी के देश में स्थापित करने की कोशिश में हैं। क्या यह संभव है?
हमें अभी भी भारत के लोक से उम्मीद है। उम्मीद है कि जिस दिन ये अन्याय अपनी हद पर पहुंचेगा, प्रतिकार के सभी झरोखे, खिड़कियां, दरवाजे एकसाथ खुल जाएंगे, चुप्पी टूटेगी, सियापा छंटेगा और लोकप्रहरी हुंकार भरेंगे। फिर फासीवाद और उसके चेलों की दुम किधर होगी, मुंह किधर होगा, हम इतिहास में ही पढ़ पाएंगे। हमें उस दिन का इंतजार है। लोभ-तंत्र के टूटने, और लोक-तंत्र के फिर से जीवंत हो उठने का।
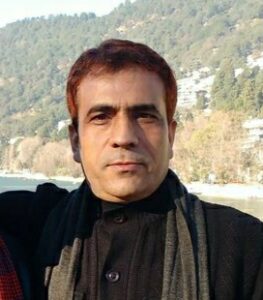
(वरिष्ठ पत्रकार सरोज कुमार इन दिनों स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं।)