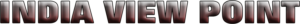सरोज कुमार
अनुपम (Anupam Mishra) यानी जैसा कोई नहीं। लेकिन अनुपम जी ऐसे भी नहीं थे। वह सभी के जैसे थे, लेकिन सभी से अलग भी थे। उनके लिए वह भी उतना ही महत्वपूर्ण, या कहीं अधिक महत्वपूर्ण था, जो सबके लिए महत्वहीन होता है। वह समाज के इस रंग से प्रभावित तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन कभी-कभी इसे लेकर उनकी चिंता बातचीत के दौरान छलक पड़ती थी।
कम लोग अपने नाम को अर्थवान कर पाते हैं। जब नाम अनुपम (Anupam Mishra) हो तो यह काम और कठिन हो जाता है। अनुपम नाम होना और अनुपम होना, ज़मीन और आसमान की ऊंचाई-निचाई की बात हो जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति का यहां ज़िक्र किया जा रहा है, वह नाम के साथ अनुपम अर्थ वाले भी थे। अनुपम होने के पीछे क्या होना होता है, क्या नहीं होना होता है और कैसे होना होता है, यह जानना-समझना हमारे जीवन की आपाधापी में काफी पीछे छूट चुका है। लेकिन जिसने इसे जान-समझ लिया, वह वाक़ई अनुपम हो जाता है।
अनुपम मिश्र को शरीर छोड़े चार साल हो चुके हैं। लेकिन लगता है वह अशरीरी होकर अपने को अधिक व्यापक रूप में अर्थवान कर रहे हैं। बाढ़-सुखाड़, पानी और पर्यावरण जब जीवन का संकट बनते जा रहे हैं तो समझिए अनुपम मिश्र इस संकट में हर क्षण समाधान बनकर सामने खड़े हैं। याद उसे करते हैं, जो अप्रासंगिक होकर भुलाया जा चुका हो। जो हर क्षण सामने खड़ा है, उसे तो बरतने की ज़रूरत है। अनुपम मिश्र को बरतना आसान भी नही है, लेकिन न बरतना कहीं अधिक कठिनाई पैदा करने वाला है। यह कोई निजी राय नहीं है, बल्कि अनुपम जी के बारे में कोई दो राय है ही नहीं। जब अनुपम जी को बरतने की बात आती है तो उनके बारे में लिखने को लेकर भी धर्मसंकट खड़ा होता है। धर्मसंकट के कारण ही चार साल तक उनपर कुछ नहीं लिखा। अनुपम जी के साथ जो धर्मसंबंध रहा है, उसके आधार पर उनके जीवनकाल में न सही, उनके बाद तो कम से कम एक आलेख बनता ही था।
अनुपम जी व्यक्ति प्रचार को पसंद नहीं करते थे। स्वयं किसी के बारे में न लिखते थे, न ख़ुद के बारे में लिखवाना चाहते थे। उन्होंने अपने पिता यानी प्रख्यात कवि पंडित भवानी प्रसाद मिश्र (Bhawani Prasad Mishra) के बारे में भी अपने पूरे जीवनकाल में सिर्फ़ एक आलेख को छोड़कर कभी कुछ नहीं लिखा। अनुपम मिश्र अपने समय के शीर्ष गद्य लेखक थे। उनकी जगह कोई दूसरा होता तो इतने प्रतिष्ठित पिता पर एक क्या कई पुस्तकें लिख चुका होता। हर साल जयंती और पुण्यतिथि मनाने के लिए कोई एक संस्था बना लिया होता। अनुपम जी ने ऐसा नहीं किया। कई सारे पत्रकार अक्सर उनसे पानी और अन्य मुद्दों पर बात करने पहुंच जाते थे। विनम्रता के साथ वह उन्हें किसी दूसरे विशेषज्ञ के पास भेज देते थे, विशेषज्ञ का पता और फोन नंबर तक उपलब्ध करा देते थे। फोन करके उसे बोल भी देते थे। लेकिन जब कोई विनती करता कि नहीं आपके बग़ैर दिक्क़त हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में वह सारा काम छोड़कर उसकी मदद भी कर देते थे। अनुपम जी ने जो कुछ लिखा, जो कुछ बोला समाज के लिए। स्वयं को आगे बढ़ाने या लेखक, वक्ता, विशेषज्ञ के रूप में स्थापित होने के लिए उन्होंने एक शब्द न लिखा, न बोला। वह जर्मन चिंतक राइनर मारिया रिल्के के उस कथ्य से शायद प्रभावित थे, जिसे उसने एक युवा कवि को लिखे अपने पत्र में कहा था- लिखे बग़ैर रह सको तो मत लिखो।
अनुपम जी ने जो भी किताबें लिखीं, चाहे वह ‘आज भी खरे हैं तालाब’ हो, ‘राजस्थान की रजत बूंदें’ हो या फिर ‘हमारा पर्यावरण’, किसी में भी ख़ुद को लेखक घोषित नहीं किया। उनकी किताबों में उनका नाम ढूढ़ने के लिए मैग्नीफ़ाइंग लेंस की ज़रूरत होती है। गांधी मार्ग (Gandhi Marg) का पुनः प्रकाशन शुरू हुआ तो उसमें भी उन्होंने अपना नाम नाममात्र का ही दिया। स्वयं को संपादक घोषित नहीं किया। कई लोगों ने इसके लिए उन्हें फोन किया कि पत्रिका में एक ग़लती जा रही है। संपादक की जगह संपादन लिखा हुआ है। अनुपम जी ने विनम्रता के साथ कहा कि “यह ग़लती नहीं है, मैं तो संपादन ही करता हूं।” अनुपम जी संज्ञा के बदले क्रिया रह कर जीना चाहते थे, और उन्होंने इसे अंतिम क्षण तक जीया। लोग जिन चीजों के लिए जीते-मरते हैं, अनुपम जी उन चीज़ों से आजीवन मुक्त रहे।
अनुपम जी के क्रिया रूप की गवाही अपने धर्मसंबंधों के कारण ही दे पा रहा हूं। उन जैसे व्यक्ति के साथ स्वयं के संबंधों के बारे में कुछ लिखने में सहज संकोच होता है, क्योंकि ऐसा करने का एक अर्थ स्वयं का बखान करना भी होता है। लेकिन यह कहने में संकोच नहीं कि हमारे संबंधों की 10 साल की अवधि में उनसे जो स्नेह मिला है, वह जीवन की अबतक की बड़ी पूंजी है।
इसे भी पढ़ें – अर्थव्यवस्था का भरोसेमंद मॉडल विकसित करने की दरकार
कई लोगों के लिए वह अनुपम जी, कई लोगों के लिए अनुपम भाई, घर के लिए पमपम थे और मेरे लिए अनुपम भैया। वर्ष 2006 में गांधी मार्ग का पुनःप्रकाशन शुरू हुआ, तो हमारी जैसे लॉटरी लग गई। मुझे गांधी मार्ग के प्रूफ़ पढ़ने की ज़िम्मेदारी मिल गई। प्रश्न प्रूफ़ पढ़ने का नहीं था, गांधी मार्ग के संपादन, प्रकाशन की पूरी प्रक्रिया से जुड़ना और अनुपम जी के साथ बैठना, उनके साथ समय बिताना अपने आप में बड़ा प्रश्न था। उन दिनों एक अख़बार के ब्यूरो में काम करता था। हर रोज़ अनुपम जी के पर्यावरण कक्ष से दो-तीन बड़ी ख़बरें मिल जाती थीं। शासन-प्रशासन के लोग अक्सर उनके पास आते रहते थे। पर्यावरण कक्ष मेरे लिए सूचना विभाग बन गया था। हर दिन पर्यावरण कक्ष पहुंचना, अनुपम जी के साथ कुछ घंटे बिताना दिनचर्या का हिस्सा था। इसी दौरान गांधी मार्ग का प्रूफ़ भी पढ़ना हो जाता था। उन्होंने मुझे प्रूफ़ पढ़ना सिखाया। प्रूफ़ पढ़ते समय किस त्रुटि के लिए क्या संकेत और कहां लगाने हैं, जिसे टाइप करने वाला समझ कर ठीक कर दे, आज के जमाने के लेखकों-पत्रकारों को कम ही पता है। कंप्यूटर की दुनिया में ऑनलाइन हो चुके शब्दों की त्रुटियां ठीक करने के लिए हालांकि इन संकेतों की अब ज़रूरत भी नहीं रह गई है। किसी दिन किसी कारणवश पर्यावरण कक्ष नहीं पहुंच पाता तो अनुपम जी का शाम को फोन आ जाता- “भैया आज आए नहीं। बस इतना जानने के लिए फोन किया कि सब कुशल तो है न।” इन शब्दों का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, सिर्फ़ अपराध बोध के सिवा। हमारा साथ पर्यावरण कक्ष तक सीमित नहीं था, बल्कि घर और बाहर के पर्यावरण तक विस्तारित था, और यह 19 दिसंबर, 2016 को असीमित हो गया। अनुपम जी के साथ रह कर जो मैंने उन्हें जाना-समझा, वह ख़ुद को कहीं अधिक जानना-समझना था। आज अपने पैर उसी समझ की बुनियाद पर खड़े हैं।

अनुपम यानी जैसा कोई नहीं। लेकिन अनुपम जी ऐसे भी नहीं थे। वह सभी के जैसे थे, लेकिन सभी से अलग भी थे। उनके लिए वह भी उतना ही महत्वपूर्ण, या कहीं अधिक महत्वपूर्ण था, जो सबके लिए महत्वहीन होता है। वह समाज के इस रंग से प्रभावित तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन कभी-कभी इसे लेकर उनकी चिंता बातचीत के दौरान छलक पड़ती थी। वह कहते थे- “देखो, वजन देने से वजन बढ़ता है। कई लोग यहां आते थे, जिनके पैरों में टूटी हवाई चप्पलें हुआ करती थीं, कैंटीन में मेरे नाम पर भोजन कर के चले जाते थे, आज वे हर माह विदेश यात्राएं कर रहे हैं। तुम्हारा जूता तो कई गुना अच्छा है।”
वाक़ई कई सारे हल्के लोग अनुपम जी के वजन से वजनी बन पाए हैं। यहां उनके नाम गिनाने में धर्मसंकट की स्थिति है। अनुपम जी ऐसे ही हल्के, नए लोगों को तलाशते, तराशते रहते थे, जिन्हें वजन देकर वजनी बनाया जा सके। जीवन के अंतिम कुछ सालों में उनकी यह तलाश, तराश तेज़ हो गई थी। उन्हें ऊंची संस्थाओं, ऊंचे हो चुके लोगों और ऊंची मान्यताओं पर से भरोसा उठ गया था। ठीक उसी तरह, जिस तरह विनोबा को भूदान की विफलता के बाद उस आंदोलन और आंदोलन से जुड़े लोगों पर से भरोसा उठ गया था। उन्होंने कहा था -बी से बाबा, बी से भूदान और बी से बोगस।
अनुपम जी को कई साल पहले ही शायद इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि उनके पास समय काफी कम बचा है। वह कई बार बात-बात में बोल जाते थे -’’अब कितना काम कराओगे भैया! उम्र भी कुछ चीज़ होती है। बहुत हो चुका, अब तुम लोग संभालो। अब तो अपना पर्दा गिरने वाला है।’’ उनकी ये बातें तूफान की तरह हिला कर रख देती थीं। मन भावुक हो उठता था। वह तुरंत विषय बदल देते थे।
अनुपम जी कई काम इस तरह कर जाते, जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता था। बाद में लोगों को लगता कि यह तो मैं भी कर सकता था। लेकिन किया तो नहीं न; यही करना ही तो होता है अनुपम बनने के लिए। अनुपम जी के साथ के अनगिनत संस्मरण हैं। यहां दो-एक का ज़िक्र करूंगा।
इसे भी पढ़ें – क्या पुरुषों का वर्चस्व ख़त्म कर देगा कोरोना?
केंद्रीय हिंदी संस्थान की तरफ़ से हिंदी में विज्ञान लेखन के लिए उन्हें पुरस्कार मिलना था। एक लाख रुपए पुरस्कार राशि थी। राष्ट्रीय राजधानी के विज्ञान भवन में पुरस्कार समारोह था। वह मुझे भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन ऑफ़िस का समय टकरा रहा था। ऑफ़िस पहुंचने के बाद हालांकि आयोजन में शामिल होने और उसकी रपट तैयार करने की ज़िम्मेदारी मुझे ही मिल गई, मन मांगी मुराद की तरह। किसी कार्यक्रम में पीछे बैठना अपनी आदत है, अनुपम जी भी ऐसा ही करते थे। इसमें सुविधा यह होती है कि एक तो आप किसी को असुविधा पहुंचाए बग़ैर कार्यक्रम से किसी भी समय आसानी से निकल सकते हैं, और दूसरे यह कि कार्यक्रम में मौजूद हर किसी को देख सकते हैं। विज्ञान भवन में भी पिछली पंक्ति में था।
पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों मिलना था। अनुपम जी कलाम को उनकी पुरा (PURA) यानी प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज़ टू रूरल एरियाज़ (Providing Urban Amenities to Rural Areas) योजना के कारण राष्ट्राध्यक्ष के रूप में पसंद नहीं करते थे। पुरा योजना बनाए जाने के दौरान योजनाकारों ने अनुपम जी से भी सलाह ली थी और उन्होंने इसे सिरे से ख़ारिज कर दिया था। यह योजना आजतक ज़मीन पर नहीं उतर पाई है। पुरा योजना के बारे में फिर कभी। फ़िलहाल पुरस्कार समारोह पर लौटते हैं। अनुपम जी पैसे को निर्दोष मानते थे, लेकिन सरकारी पैसे से वह हमेशा दूर रहते थे। यहां तक कि कई सरकारी कमेटियों के अध्यक्ष रहने के दौरान निर्धारित मानदेय तक नहीं लेते थे। सरकारी कारें लौटा देते थे और बस या ऑटो लेकर बैठकों में पहुंचते थे। भौतिक जीवन में पैसे के प्रति ऐसा निर्लोभी मैंने नहीं देखा, जिसने अपनी पुस्तकों पर कॉपीराइट तक नहीं रखा। स्नेह के साथ हालांकि कोई पुरस्कार राशि देता तो विनम्रता से स्वीकार लेते थे और उसमें से थोड़ा अपने पास रखकर बाक़ी गांधी शांति प्रतिष्ठान (Gandhi Peace Foundation) को सौंप देते थे। लेकिन प्रशस्ति-पत्रों में उन्होंने कभी प्रशस्ति नहीं देखी। प्रशस्ति-पत्र उनके लिए कबाड़ की वस्तु थे। हां, कोई अच्छा फ्रेम होता था तो उसमें पर्यावरण से जुड़ा या अन्य कोई कलात्मक चित्र चिपका कर उसे घर की दीवार पर टांग देते थे।
केंद्रीय हिंदी संस्थान पुरस्कार के निर्णायक मंडल के सदस्य अनुपम जी के स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उन्होंने पहले ही बातचीत करके उन्हें पुरस्कार लेने के लिए राजी कर लिया था, उसके बाद ही नाम की घोषणा की थी। राष्ट्रपति के हाथों कोई पुरस्कार दिया जाता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। पुरस्कार लेने वाला कब सभा कक्ष में पहुंचेगा, उसकी सीट कहां होगी, पुरस्कार लेने के लिए किस तरफ़ से वह जाएगा, सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। सारी चीजों का समारोह से पहले अभ्यास भी किया जाता है। अनुपम जी प्रोटोकॉल के अनुसार अपनी सीट पर बैठे हुए थे। इसी बीच उनकी नज़र अचानक मुझ पर पड़ गई और वह अग्रिम पंक्ति से उठ कर सीधे पीछे मेरे पास आ गए। “आप! बहुत अच्छा; तो ऑफ़िस वालों ने आपको यहां भेज दिया।”
अनुपम जी मेरे बग़ल वाली कुर्सी पर बैठ गए और विनोदपूर्ण अंदाज़ में बातें करने लगे। “देखो, आयोजन से अपन को क्या लेना-देना, बस कलाम साहब से लिफ़ाफ़ा ले लो और यहां की जलेबी खाकर खिसक लो। पता है न, यहां की जलेबी बहुत अच्छी होती है। बग़ैर खाए मत जाना, खाना भी अच्छा होता है। अपन साथ में निकलेंगे।” अनुपम जी ने बैठे-बैठे विज्ञान भवन के बारे में, वहां के भोजन, नाश्ते की गुणवत्ता के बारे में, और ऐसे आयोजनों के बारे में न जाने कितनी जानकारी दे दी। वह सारे प्रोटोकॉल को दरकिनार कर तब तक मेरे पास ही बैठे रहे, जब तक कि उद्घोषक ने उनके नाम की घोषणा नहीं कर दी। क्या कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा कर सकता है? इसे कोई अनुपम ही कर सकता है।
अनुपम जी किसी चीज़ के प्रति आग्रही नहीं होते थे, निराग्रही भी नहीं, दुराग्रह तो कोसों दूर की बात थी उनके लिए। अधिकार शब्द से उन्हें बहुत चिढ़ थी, वह अधिकार पाने के लिए की जाने वाली किसी कोशिश, आंदोलन से अलग रहते थे। वह सिर्फ़ काम करने का अधिकार जानते थे, जिसे ईश्वर ने सभी को देकर धरती पर भेजा है। इसमें न तो किसी को देना है, और न किसी से कुछ लेना है; न जीतना है, न हारना है; बस काम करते जाना है। यही गांधी मार्ग भी है, अनुपम जी के जीवन का मार्ग यही था। अपनी पुस्तक ’आज भी खरे हैं तालाब’ में उन्होंने लिखा भी है -’’बस अच्छे-अच्छे काम करते जाओ।’’ वह अक्सर यह भी कहते थे -’’देखो, काम तो करने से ही होगा, अधिकार मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है।’’
अनुपम मिश्र कबीर के ’’बिन मांगे मोती मिले…’ की सोच के साधक थे। जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने इस साधना को जारी रखा।
अनुपम जी अनाग्रही थे, इसलिए वह अजातशत्रु भी थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनकी बुराइयां करने वाले नहीं थे। जिनके काम नहीं सध पाते, वे उनकी बुराइयां करने लगते थे। अनुपम जी को सब पता रहता था, लेकिन वह ऐसे लोगों के साथ भी समान रूप से सहज भाव रखते थे, और भविष्य में उनकी मदद भी करते थे। फिर वही व्यक्ति उनका प्रशंसक बन जाता था। कई लोग ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान भी किया; वह कुछ क्षण के लिए दुखी भी हो जाते थे, लेकिन ऐसे लोगों के साथ भी उन्होंने कभी प्रतिशोध का भाव नहीं रखा, अलबत्ता उनका दिल जीतने की कोशिश की। वह कहते थे- “अच्छे लोगों के साथ काम तो कोई भी कर सकता है, फिर समाज के बुरे लोगों का क्या होगा, इनके साथ काम कौन करेगा? हो सकता है ऐसे लोगों के साथ काम करने से वे अच्छे बन जाएं।’’
बीमारी की जानकारी सामने आई तो उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में मिलने पहुंचा तो अपना मन भावुक था। लेकिन अनुपम जी को यहां भी विनोद सूझा हुआ था। अपना हाल-चाल, अपनी बीमारी भूलकर वह अस्पताल की इमारत और वहां की व्यवस्था का बखान करने लगे। “अस्पताल कितना सुंदर बना है। यहां का रेस्तरां बहुत अच्छा है। आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है यहां की। जाओ तुम लोग एक-एक आइसक्रीम तो खा ही लो। संदीप (प्रभाष जोशी जी के बड़े पुत्र संदीप जोशी) जाओ जरा रेस्तरां से होकर आओ, और स्वाद मुझे भी बताना।’’ उनकी ये बातें सुनकर आंखें छलछला उठीं। लेकिन वह तो मुस्कुरा रहे थे। न चाहते हुए भी बेमन से संदीप जी के साथ रेस्तरां जाना पड़ा, लेकिन कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने फिर भी ज़िद की “नहीं, चाचा ने कहा है तो अपन को लेना ही पड़ेगा, स्वाद भी उन्हें बताना है।’’
इलाज कराने के बाद जब वह पहली बार घर लौटे, तो मिलने गया था। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा -’’देखो डॉक्टर तो कह रहे हैं कि रपट नॉर्मल है, ठीक हो गया है, लेकिन इस बीमारी का कोई ठिकाना नहीं, कब पलटी मार जाए, तुम लोग भी मन मज़बूत कर के रखो। लेकिन जब तक हैं, काम करेंगे, और ख़ूब काम करना है।’’
गीता के अध्याय तीन, चार और आठ में कर्म के मर्म के बारे में लिखा है- “कर्म करना मनुष्य की प्रकृति में निहित है; आलस्य हिंसा के अलावा और कुछ नहीं है।’’ तो अनुपम जी के बारे में कह सकते हैं कि उन्होंने गीता के इस मर्म को कर्म में बदल दिया था। वह आजीवन अहिंसक बने रहे। एक सच्चा कर्मयोगी!
अनुपम जी के मूल्य अपने थे, इसीलिए वह अमूल्य थे। उन्हें किसी मूल्यवान की ज़रूरत नहीं होती थी। उनके पास किसी भी वस्तु, विषय को मूल्यवान बनाने का कौशल था। उनका जीवन उनके इर्द-गिर्द के वातावरण, संसाधनों से चलता था। उनकी पूंजी यही थी। जिन लोगों ने उनके पर्यावरण कक्ष को देखा है, वे इस बात को जानते हैं। अपनी टूटी-सी आलमारी पर जब उन्होंने कोलाज बनाया तो वह कीमती कलाकृति बन गई, आकर्षण की वस्तु बन गई। न जाने कितनों ने उसकी तस्वीरें उतारी होंगी, तस्वीरें पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई होंगी। इसी तरह उनके कक्ष में कई-सारी ऐसी वस्तुएं रहीं हैं, जो अनुपम स्पर्श से अनुपम बनी हैं।
गांधी मार्ग के संपादन के लिए उन्होंने कभी कोरे काग़ज़ का इस्तेमाल नहीं किया। वह ‘कारे कागद’ पर ही उजली इबारतें लिखते रहे। वे इबारतें संपादन की मिसाल बन चुकी हैं। रोज की डाक से निकलने वाली रद्दी उनके लिए ‘ज्ञान आयोग’ था। पूरा संपादन कार्य उसी ’ज्ञान आयोग’ पर होता था; ज़रूरत पड़ने पर ज्ञान आयोग से कुछ रद्दी मैं भी निकाल लाता था। अनुपम जी के संपादन कौशल की बात फिर कभी। फ़िलहाल ज्ञान आयोग पर आते हैं। ज्ञान आयोग का गठन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने किया था। सैम पित्रोदा (Sam Pitroda) उसके अध्यक्ष थे। आयोग की किसी बैठक में अनुपम जी भी गए थे; वहां से ज्ञान कितना निकला यह तो नहीं पता, लेकिन एक अनूठा विज्ञान ज़रूर हाथ लग गया। अनुपम जी बैठक से एक अच्छी-मोटी फ़ाइल लेकर आए थे। एक बार मुझे कुछ रद्दी की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कहा- वह ज्ञान आयोग उठाओ। उन्होंने उसमें से कुछ पन्ने निकाल कर दिए और कहा- “यह आयोग इसी काम का है।’’ उन्होंने यक्ष प्रश्न भी खड़ा किया- “अब सरकार ने ज्ञान आयोग बनाया है, यानी अभी तक सारे काम अज्ञान आयोग से चल रहे थे!’’
उसी दिन से ज्ञान आयोग की फ़ाइल पर्यावरण कक्ष में रद्दी का पर्याय बन गई। हम रद्दी को ज्ञान आयोग के नाम से ही बुलाने लगे थे। आगे चलकर अनुपम जी की बात सच साबित हुई। ज्ञान आयोग वाक़ई रद्दी से ज़्यादा कुछ साबित नहीं हो पाया। लेकिन अनुपम जी उसी रद्दी पर आजीवन ज्ञान-विज्ञान की अमर कथा लिखते रहे। उनके बहुत सारे काम उसी रद्दी से हो जाते थे। वह देश-विदेश कही भी होते, जेब में बटुआ रद्दी से ही बना होता था। जब रद्दी का बटुआ बिल्कुल रद्दी हो जाता था, तो किसी नई रद्दी का नंबर आता और अनुपम जी उस रद्दी से नया बटुआ बना लेते थे। उनकी मेज़ पर चाय की प्याली रखने की चट्टी हो, या कलम-पेंसिल, कटर रखने का बरतन, सब रद्दी का ही होता था। उनके इस कला की मांग भी थी। कई लोग आग्रह करते तो वह सहज रूप में बना कर दे भी देते थे।
गांधी शांति प्रतिष्ठान से दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अक्सर शाम को बंगाली मार्केट जाते थे। कई बार हम साथ होते थे। एक दिन बंगाली मार्केट से ख़रीदारी के बाद हम राजघाट के लिए बस पकड़ने पैदल मंडीहाउस की तरफ़ लौट रहे थे। रास्ते में लाल पत्थर का एक टुकड़ा दिख गया। पता नहीं कितने दिनों से वहां पड़ा था। पत्थर का टुकड़ा क्या, किसी प्रस्तर स्तंभ का सुंदर आकर्षक शिखर कमल था, बिल्कुल तराशा हुआ। अनुपम जी की नज़र उस पर पड़ी, वह रुक गए।’’ बड़ा सुंदर पत्थर है, यहां बेकार पड़ा है, इसे तो आज ले चलते हैं।’’ उन्होंने मुझे झोला पकड़ाया और सारा सामान दुकानदार से मिले थैले में रख लिया और पत्थर को झोले में। वह पत्थर उनके घर के सामने छोटी-सी बगिया का सदस्य बन गया। अनुपम स्पर्श से उस पत्थर का अहिल्या उद्धार हो गया।
इसे भी पढ़ें – क्षमा बड़न को चाहिए…
अनुपम जी का जीवन बिल्कुल सरल था, लेकिन ऐसा नहीं कि कठिन जीवन वालों से वह संपर्क-संबंध नहीं रखते थे। कठिन से कठिन जीवनशैली वाले भी उनसे मिलने के बाद अपने भीतर सरलता और तरलता का अनुभव करते थे। आधुनिकतम दुनिया से लेकर गांव-गिरांव तक के लोग उनके समाज का हिस्सा थे। अनुपम जी के पास हर किसी के लिए कुछ न कुछ था। उनसे मिलकर कोई निराश नहीं लौटता था। चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, कला का व्यक्ति हो या साहित्य का, विज्ञान का हो या मनोविज्ञान का, संगीत का हो या दर्शन का, अनुपम जी के दर्शन से हर कोई तृप्त-संतृप्त हो जाता था। वह सहज ही सभी से घुल-मिल जाते थे।
उनका प्रिय विषय पानी था, लेकिन उस पानी में जीवन के तमाम विषय घुले हुए थे, जो समय-समय पर उतराते रहते थे। कोई चाहे तो गोता लगाकर अपनी पसंद का मोती निकाल सकता था। उन्होंने अपने एक लेख में ‘भाषा और पर्यावरण’ की अनुपम जुगलबंदी पेश की है। एक आग्रही मित्र के आग्रह पर उन्होंने ’पुरखों से संवाद’ का अद्भुत दर्शन पेश किया है। इसी तरह एक अन्य मित्र के आग्रह पर मृत्यु से साल भर पहले उन्होंने ‘जीवन का अर्थ और अर्थमय जीवन’ विषय पर अद्भुत व्याख्यान दे डाला था। वह व्याख्यान आलेख के रूप में प्रकाशित भी हुआ है। व्याख्यान में उन्होंने जो बातें कही हैं, वे जीवन के मूर्त और अमूर्त रूपों-पक्षों की सटीक सांख्यिकी प्रस्तुत करती हैं। यह उनके जीवन का अंतिम व्याख्यान था, जिसका मैं भी साक्षी था।
महाराष्ट्र के वर्धा में 22 दिसंबर, 1947 को अवतरित हुए इस अनुपम ऋषि की सहज, सरल जीवनशैली के नाते कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उन्हें कोई बीमारी होगी। लेकिन इस कर्मयोगी के शरीर का अंत कैंसर जैसी बीमारी से! यह जानकर हर किसी को सदमा लगा था। लगता है अनुपम जी यहां भी कुछ अनुपम ही करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हमारी सामान्य सोच के साथ साज़िश रची थी। उन्होंने शरीर त्यागने का अनुपम रास्ता चुन लिया था। संवभतः वह कहना चाह रहे थे -’’देख लो, जब मेरे जीवन का पर्यावरण इस तरह बिगड़ सकता है, तो आज के वातावरण में तुम लोगों को कम से कम अब सावधान हो जाना चाहिए।’’
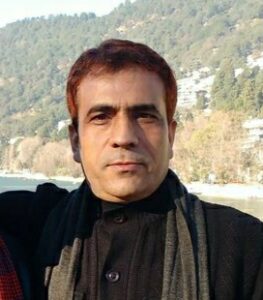
(वरिष्ठ पत्रकार सरोज कुमार इन दिनों दिल्ली में स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। उनका यह लेख न्यूज़18 की वेबसाइट से साभार लिया गया है।)
Share this content: