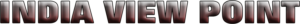हरिगोविंद विश्वकर्मा
अपनी जन्मभूमि से लगाव मानव का स्वाभाविक आदत होती है। इसीलिए हर आदमी जीवन भर उस स्थान को मिल करता है, जहां वह पैदा हुआ होता है और पला-बढ़ा होता है। दरअसल, इंसान अपनी जन्मभूमि से जीवन भर भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है। यही भावनात्मक आदत ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार (Tragedy King Dilip Kumar) को पाकिस्तान से भावनात्मक रूप से जोड़े थी। चूंकि भारत पाकिस्तान के बीच कई जंग हो चुकी है। इसलिए किसी भारतीय नागरिक का पाकिस्तान के बारे में कोई सकारात्मक बात भी नकारात्मक ढंग से प्रचारित की जाती है। यही दिलीप कुमार के साथ भी हुआ, जब बार-बार लोग उनका नाम पाकिस्तान से जोड़ देते थे।
दरअसल, दिलीप कुमार का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। इसलिए पाकिस्तान खासकर पेशावर से उनका उसी तरह का भावनात्मक लगाव था, जिस तरह पाकिस्तान के क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना (Mohammad Ali Jinnah) का भावनात्मक लगाव मुंबई से था। दरअसल, देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार जिन्ना पाकिस्तान बनने के बाद भले पाकिस्तान में रह रहे थे, लेकिन वह मलाबार हिल के अपने घर जिन्ना हाउस का बहुत मिस करते थे। कहते हैं कि उनका दिल मुंबई में ही रह गया था। जिन्ना की पत्नी रुतिन की मजार मुंबई में थी। पाकिस्तान में होने की वजह से वह उस मजार पर जा नहीं सकते थे। इसका मलाल उन्हें ज़िंदगी भर रहा। इसी तरह पाकिस्तान का ज़िक्र होने पर दिलीप कुमार भावुक हो जाते थे।
यही वजह है कि जब 1998 में पाकिस्तान सरकार ने दिलीप कुमार को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘निशान-ए-इम्तियाज’ (Nishan-E-Imtiaz) से सम्मानित किया, तो उस पर भारत में जमकर राजनीति हुई थी। सत्ता सुख भोगने के लिए आजकल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलाने के बाद सेक्यूलर चोला पहनने वाली शिवसेना उस समय दिलीप कुमार पर हमले पर हमला कर रही थी। शिवसेना के मुखपत्र में दिलीप कुमार द्वारा पाकिस्तानी सम्मान स्वीकार किए जाने पर उनकी देशभक्ति पर सवाल भी उठाए गए थे। लेकिन दिलीप कुमार वर्ष 1999 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के परामर्श के बाद ‘निशान-ए-इम्तियाज’ पुरस्कार को बरकरार रखा।
भारत के अलावा पाकिस्तान में भी दिलीप कुमार के काफी चाहने वाले हैं। एक और किस्सा है जो बताता है कि दिलीप कुमार भावनात्मक रूप पाकिस्तान से कितना जुड़े थे। यह यह दिलचस्प वाकया सन् 1999 मेंके कारगिल जंग से जुड़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कार्यकाल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे खुर्शीद कसूरी की किताब ‘नीदर ए हॉक नॉर ए डव,’ में इस वाकये का जिक्र है। मई 1999 में संघर्ष को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे। इस किताब में लिखा है कि संघर्ष के दौरान जब लीजेंड्री एक्टर दिलीप कुमार ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्रि नवाज से बात की तो हर कोई चौंक गया था। कसूरी ने अपनी इस किताब में कारगिल युद्ध के समय पीएम के प्रधान सचिव सेक्रेटरी रहे सईद मेहदी के हवाले से इस घटना को लिखा है।
एक दिन समय वह शरीफ के साथ बैठे थे कि अचानक फोन की घंटी बजी। शरीफ के एडीसी ने बताया कि इंडियान पीएम वाजपेयी उनसे तुरंत बात करना चाहते हैं। वाजपेयी ने कायत की कि लाहौर में बुलाने के बाद इतना बड़ा धोखा दिया। वाजपेयी की बात सुनकर शरीफ हैरान थे। शरीफ को जरा भी इल्म नहीं था कि वाजपेयी उनसे क्या कह रहे हैं। उन्होंने वाजपेयी से वादा किया कि आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ से बात करके वह उन्हें दोबारा कॉल करेंगे। बात खत्म होती इससे पहले वाजपेयी ने शरीफ से कहा कि वह चाहते हैं कि वह दिलीप कुमार साहब से बात करें। दिलीप कुमार ने फोन पर उनसे कहा, ‘मियां साहब, हमने आप से यह उम्मीद नहीं की थी। आप तो हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती की बात करते आए हैं।’ दिलीप कुमार ने शरीफ से कहा कि तनाव की वजह से भारतीय मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वे अपने घरों को छोड़ने में कई तरह के डर और मुश्किलों को महसूस कर रहे हैं। ऐसे में यह शरीफ की जिम्मेदारी है कि हालात पर काबू करें।
बहरहाल, दुनिया उन्हें भले दिलीप कुमार के नाम से जानती है। भले उनके अभिनय की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन सच यह है कि उनकी न तो फ़िल्मों में काम करने की दिलचस्पी थी और न ही उन्होंने कभी सोचा था कि दुनिया कभी उन्हें मोहम्मद युसुफ़ खान की बजाए दिलीप कुमार के नाम से याद करेगी। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा ‘द सबस्टांस एंड द शैडो’ (The Substance And The Shadow) में अपने जन्म से लेकर अभिनय की बुलंदियों पर पहुंचने तक के सफर के अपने इन अनुभवों को बखूबी पेश किया है। 11 दिसंबर, 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे दिलीप कुमार के बचपन मोहम्मद युसुफ़ खान था। उनके पिता मोहम्मद सरवर ख़ान मुंबई में फलों के बड़े कारोबारी थे, लिहाजा शुरुआती दिनों से ही दिलीप कुमार को अपने पारिवारिक कारोबार में शामिल होना पड़ा। एक दिन किसी बात पर पिता से झगड़ा हो गया और दिलीप कुमार मुंबई से पुणे चले गए। अंग्रेजी की अच्छी जानकारी होने के चलते उन्हें पुणे के ब्रिटिश आर्मी के कैंटीन में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई और वह अपने पांव पर खड़े हो गए।
बाद में पुणे में उन्होंने अपना सैंडविच काउंटर खोला जो अंग्रेज सैनिकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गया था, लेकिन इसी कैंटीन में एक दिन किसी आयोजन के सिलसिले में भारत की आज़ादी की लड़ाई का समर्थन करने के चलते उन्हें गिरफ़्तार होना पड़ा। इसके बाद उनका काउंटर बंद हो गया। आजीविका छिनने के बाद यूसुफ़ ख़ान फिर से बंबई (अब मुंबई) लौट आए और पिता के काम में हाथ बंटाने लगे। उन्होंने तकिए बेचने का काम भी शुरू किया जिसमें कामयाब नहीं मिली। पिता ने नैनीताल जाकर सेव का बगीचा ख़रीदने का काम सौंपा तो यूसुफ़ महज एक रुपए की अग्रिम भुगतान पर समझौता कर आए। हालांकि इसमें बगीचे के मालिक की भूमिका ज़्यादा थी, लेकिन यूसुफ़ को पिता की जमकर शाबाशी मिली।
संघर्ष के दिनों में आमदनी बढ़ाने के लिए ब्रिटिश आर्मी कैंट में लकड़ी से बनी कॉट सप्लाई करने का काम पाने के लिए यूसुफ़ ख़ान को एक दिन दादर जाना था। वह चर्चगेट स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। वहीं अचानक उनके परिचित साइकोलॉजिस्ट डॉ. मसानी मिल गए। डॉ. मसानी ‘बॉम्बे टॉकीज’ (Bombay Talkies) की मालकिन देविका रानी से मिलने जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ़ ख़ान से आग्रह किया कि चलो मुमकिन है, तुम्हें भी वहां कोई न कोई काम मिल जाए। पहले तो यूसुफ़ ख़ान ने मना कर दिया लेकिन किसी मूवी स्टूडियो में पहली बार जाने के आकर्षण के चलते वह तैयार हो गए। दोनों ने लोकल पकड़ ली।
उस समय तक दिलीप कुमार को मालूम नहीं था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। बॉम्बे टॉकीज़ उस दौर की देश की सबसे कामयाब फ़िल्म प्रॉडक्शन हाउस था। उसकी मालकिन देविका रानी स्टार अभिनेत्री होने के साथ साथ अत्याधुनिक और दूरदर्शी महिला थीं। ‘द सबस्टैंस एंड द शैडो’ के मुताबिक, जब वे लोग उनके केबिन में पहुंचे तब उन्हें देविका रानी बहुत गरिमामयी भारतीय महिला लगीं। डॉ. मसानी ने दिलीप कुमार का परिचय कराते हुए देविका रानी से उनके लिए काम की बात की। देविका रानी ने जब दिलीप कुमार से पूछा कि क्या उन्हें उर्दू आती है तो उन्होंने हां में जवाब दिया। उससे पहले ही डॉ. मसानी देविका रानी को पेशावर से मुंबई पहुंचे उनके परिवार और फलों के कारोबार के बारे में बताने लगे।
बातचीत के दौरान ही देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा कि वह अभिनय करना पसंद करेंगे? इस सवाल के साथ साथ देविका रानी ने उन्हें 1250 रुपए मासिक की नौकरी ऑफ़र कर दी। डॉ. मसानी ने दिलीप कुमार को इसे स्वीकार कर लेने का इशारा किया। लेकिन दिलीप कुमार ने देविका रानी को ऑफ़र के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके पास ना तो काम करने का अनुभव है और ना ही सिनेमा की कोई समझ। लिहाज़ा, इस प्रस्ताव को कैसे स्वीकार कर सकते हैं।
हाज़िर-जवाब देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा था कि आप फलों के कारोबार के बारे में कितना जानते हैं। उस पर दिलीप कुमार का जवाब था, “जी, मैं सीख रहा हूं।” इस पर देविका रानी ने तपाक से कहा कि जब फलों के कारोबार और फलों की खेती के बारे में सीख रहे हैं तो फ़िल्म मेकिंग और अभिनय भी सीख लेंगे। देविका रानी ने कहा, “मुझे एक युवा, गुड लुकिंग और एजुकेटेड एक्टर की ज़रूरत है। मुझे तुममें एक अच्छा एक्टर बनने की योग्यता दिख रही है।” सन् 1943 में 1250 रुपये कितनी बड़ी रकम थी, इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि दिलीप कुमार को लगा कि यह सालाना ऑफ़र है। लिहाज़ा, उन्होंने डॉ. मसानी से इसे दोबारा कंफ़र्म करने के लिए कहा और जब डॉ. मसानी ने देविका रानी से कंफ़र्म करके उन्हें बताया कि 1250 रुपए वेतन मासिक है, तब भी दिलीप कुमार को एक बार यक़ीन ही नहीं हुआ। बहरहाल, देविका रानी के इस ऑफ़र को स्वीकार करके दिलीप कुमार बॉम्बे टॉकीज़ के अभिनेता बन गए।
दिलीप कुमार की पहली फ़िल्म ‘ज्वार भाटा’ थी, जो 1944 में आई।1949 में बनी फ़िल्म ‘अंदाज़’ की सफलता ने उन्हें सिनेमा जगत में स्थापित कर दिया। इस फ़िल्म में उन्होने राज कपूर के साथ काम किया था। बहरहाल, 1950 में आई ‘बाबुल’ फिल्म में दिलीप कुमार ने पोस्ट मास्टर का रोल निभाया था। दिलीप कुमार बॉम्बे टॉकीज़ में शशिधर मुखर्जी और अशोक कुमार के अलावा दूसरे नामचीन लोगों के अभिनय की बारीकियां सीखने लगे। इसके लिए उन्हें प्रतिदिन दस बजे सुबह से छह बजे तक स्टूडियो में होना होता था।
एक दिन जब वह सुबह स्टुडियो पहुंचे तो उन्हें संदेशा मिला कि देविका रानी ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया है। इस मुलाकात के बारे में दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, “उन्होंने अपनी शानदार अंग्रेजी में कहा- यूसुफ़ मैं तुम्हें जल्द से जल्द एक्टर के तौर पर लॉन्च करना चाहती हूं। ऐसे में यह विचार बुरा नहीं है कि तुम्हारा एक स्क्रीन नेम हो। ऐसा नाम जिससे दुनिया तुम्हें जानेगी और ऑडियंस तुम्हारी रोमांटिक इमेज को उससे जोड़कर देखेगी। मेरे ख़याल से दिलीप कुमार अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी तो ये नाम अचानक मेरे दिमाग़ में आया। तुम्हें यह नाम कैसा लग रहा है?”
देविका रानी की बात सुनकर उनकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि नई पहचान के लिए वह बिलकुल तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने देविका रानी को कहा कि नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन क्या ऐसा करना वाक़ई ज़रूरी है?देविका रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, “ऐसा करना बुद्धिमानी भरा होगा। काफ़ी सोच विचारकर इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम्हारा स्क्रीन नेम होना चाहिए।” दिलीप कुमार से पहले देविका रानी अपने पति हिमांशु राय के साथ मिलकर कुमुदलाल गांगुली को 1936 में ‘अछूत कन्या’ फ़िल्म से अशोक कुमार के तौर पर स्थापित कर चुकी थीं। वर्ष 1943 में अशोक कुमार की फ़िल्म ‘किस्मत’ सुपर डुपर हिट हुई थी। इस फ़िल्म की कामयाबी ने अशोक कुमार को देखते ही देखते सुपरस्टार बना दिया था। अशोक कुमार भारतीय सिनेमा के पहले कुमार थे। ऐसे में बहुत संभव है कि ‘किस्मत’ फ़िल्म से होने वाली कमाई को देखते हुए यूसुफ़ के लिए स्क्रीन नेम का ध्यान आते वक्त देविका रानी के दिमाग़ में कुमार सरनेम क्लिक किया हो।
देविका रानी ने कहा कि वह फ़िल्मों में मेरा लंबा और कामयाब करियर देख पा रही हैं, ऐसे में स्क्रीन नेम अच्छा रहेगा और इसमें एक सेक्युलर अपील भी होगी। हालांकि ये भारत की आज़ादी से पहले का दौर था और उस वक्त हिंदू और मुस्लिम को लेकर समाज में बहुत कटुता की स्थिति नहीं थी, लेकिन कुछ सालों के भीतर ही भारत और पाकिस्तान के बीच हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंटवारा हो गया। दरअसल, देविका रानी को बाज़ार की समझ थी, उन्हें मालूम था कि किसी ब्रैंड के लिए दोनों समाज के लोगों की बीच स्वीकार्यता की स्थिति ही आदर्श स्थिति होगी। हालांकि ऐसा नहीं था केवल मुस्लिम कलाकारों को अपना नाम बदलना पड़ा रहा था और स्क्रीन नेम रखना पड़ रहा था।
यूसुफ़ ख़ान के तौर पर वे देविका रानी के तर्कों से सहमत तो हो गए लेकिन उन्होंने इस पर विचार करने का वक़्त मांगा। देविका रानी ने कहा कि ठीक है, विचार करके बताओ, लेकिन जल्दी बताना। देविका रानी के केबिन से निकल कर दिलीप कुमार स्टूडियो में काम करने लगे लेकिन उनके दिमाग़ में नया नाम ही चल रहा था। ऐसे में शशिधर मुखर्जी ने उनसे पूछ लिया कि किस सोच विचार में डूबे हो। तब दिलीप कुमार ने देविका रानी से हुई बातचीत के बारे में उन्हें बता दिया. एक मिनट के लिए ठहर कर शशिधर मुखर्जी जो उनसे कहा, “मेरे ख़्याल से देविका रानी ठीक कह रही हैं। उनका प्रस्ताव स्वीकार करना फ़ायदे का सौदा होगा। यह बहुत ही अच्छा नाम है। यह दीगर बात है कि मेरे लिए तुम युसूफ़ ही रहोगे।” इस सलाह के बाद यूसुफ़ ख़ान ने दिलीप कुमार के स्क्रीन नेम को स्वीकार कर लिया और अमिय चक्रवर्ती के निर्देशन में ‘ज्वार भाटा’ की शूटिंग शुरू हो गई।
सन् 1944 में प्रदर्शित ज्वार भाटा फ़िल्म के साथ ही भारतीय फ़िल्म इतिहास को दिलीप कुमार मिल गए। दुर्भाग्य से पहली फ़िल्म नहीं चली। ज्वार भाटा की रिलीज़ पर उस वक्त हिंदी फ़िल्मों पर नज़र रखने वाली प्रमुख पत्रिका ‘फ़िल्म इंडिया’ के संपादक बाबूराव पटेल ने लिखा, “फ़िल्म में लगता है किसी मरियल और भूखे दिखने वाले शख़्स को हीरो बना दिया गया है।” लेकिन लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका सिने हेराल्ड में पत्रिका के संपादक बीआर चोपड़ा ने दिलीप कुमार की अभिनय क्षमता को भांप लिया था। उन्होंने अपनी पत्रिका में इस फ़िल्म के बारे में लिखा कि दिलीप कुमार ने जिस तरह से इस फ़िल्म में डॉयलॉग डिलेवरी की है, वह उन्हें दूसरे अभिनेताओं से अलग करता है। फ़िल्म भले नहीं चली लेकिन देविका रानी के अनुमान के मुताबिक ही दिलीप कुमार का सितारा बुलंदियों पर पहुंचकर रोशन होता रहा।
वर्ष 1951 में आई ‘दीदार’ में अशोक कुमार के साथ नए नाम दिलीप कुमारके रूप में अभिनय किया। इस फिल्म में उन्होंने एक नेत्रहीन व्यक्ति का किरदार निभाया था। दीदार में दिलीप कुमार के किरदार ने उन्हें हिंदी सिनेमा में ट्रैजेडी किंग के रूप में स्थापित कर दिया था। दिलीप कुमार को लेकर जो सेक्युलर भाव का सपना देविका रानी ने देखा था, वह कितना वास्तविक था और दिलीप कुमार अपने अभिनय से किस तरह से सेक्युलर भाव का चेहरा बने इसे ‘गोपी’ फिल्म में मोहम्मद रफी के गाए भजन ‘सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई’ में अभिनय करते हुए उन्हें देखकर बखूबी होता है। दिलीप कुमार ने जिन 60 से ज़्यादा फ़िल्मों में अभिनय किया, उसमें केवल ‘मुगल-ए-आज़म’ में वह मुस्लिम क़िरदार में रूपहले परदे पर दिखे।
इसके अलावा उन्होंने प्रतिमा (1945), नौका डूबी (1947), जुगनू (1947), शहीद (1948), नदिया के पार (1948), मेला (1948), घर की इज्जत (1948), अनोखा प्यार (1948) ,अंदाज (1949), शबनम (1949), आरजू (1950), बाबुल (1950), जोगन (1950), हलचल (1951), तराना (1951), आन (1952), दाग (1952), संगदिल (1952), फुटपाथ (1953). शिक्स्त (1953), अमर (1954), आजाद (1955), देवदास (1955), इंसानियत (1955), उडन खटोला (1955), मुसाफिर (1957), नया दौर (1957), मधुमती (1958), यहहदी (1958), पैगाम (1959), मुगल-ए-आज़म (1960), कोहिनूर (1960), गंगा जमुना (1961), लीडर (1964), दिल दिया दर्द लिया (1966), राम और श्याम (1967), आदमी (1968), साधु और शैतान (1968), संघर्ष (1968), गोपी (1970), सगीना महातो (1970), अनोखा मिलन (1972), दास्तान (1972), कोशिश (1972), फिर कब मिलोगी (1974), सगीना (1974), बैराग (1976), क्रांती (1981), शक्ति (1982), विधाता (1982), मज़दूर (1983), मशाल (1984), दुनिया (1984), कर्मा (1986), धर्म अधीकारी (1986), कानून अपना अपना (1988), आग का दरिया (1990), इज्जतदार (1990), सौदागर (1991)और कीला (1998)
1970, 1980 और 1990 के दशक में फिल्मों में अभिनय करने का उनका सफ़र चलता रहा। 1998 में बनी फ़िल्म किला उनकी आखरी फ़िल्म थी। दिलीप कुमार ने रमेश सिप्पी की फ़िल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया। दिलीप कुमार को आठ बार 1954 में दाग, 1956 में आज़ाद, 1957 में देवदास, 1958 में नया दौर, 1961 में कोहिनूर, 1965 में लीडर, 1968 में राम और श्याम और 1983 में शक्ति में असाधारण अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार मिला। 2014 में उन्हें किशोर कुमार सम्मान दिया गया।
ऐसे समय जब लोग उम्मीद कर रहे थे कि दिलीप कुमार जीवन का शतक लगाएंगे। तभी 7 जुलाई को 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह पिछले कुछ दिनों से उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे और उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ा था। उन्हें 30 जून को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उनकी पत्नी सायरा बानो अंत समय में भी उनके साथ थीं।