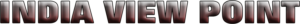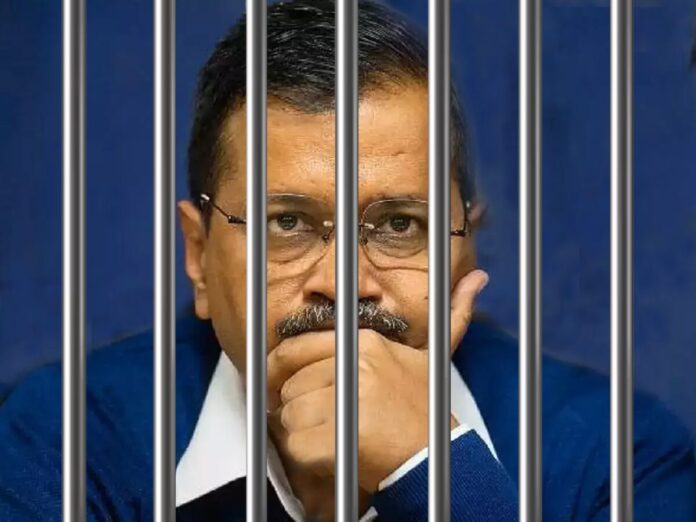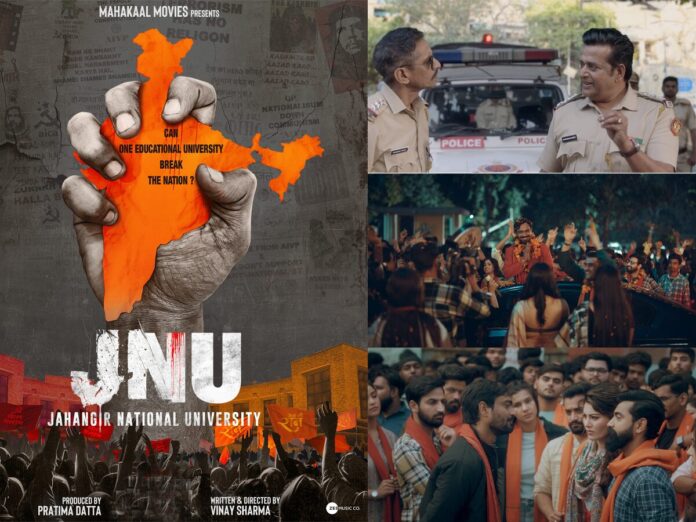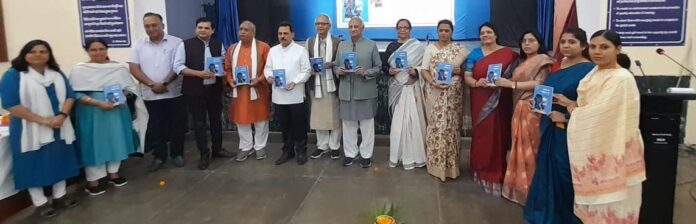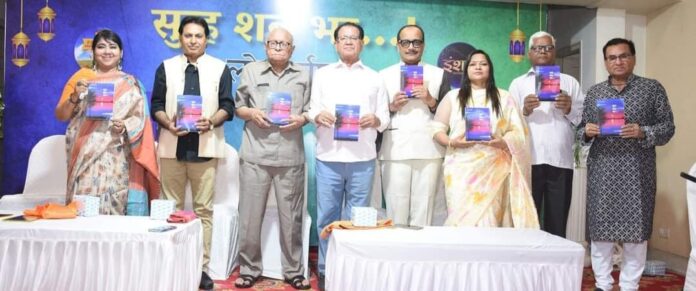विश्व क्षय रोग दिवस, 24 मार्च पर विशेष लेख
देश के लिए ख़ुशी की बात यह है कि देश में टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई मरीज़ों की संख्या तेज़ी से घट रही है, फिर भी 2025 तक भारत को टीबी-मुक्त करने का लक्ष्य कठिन जान पड़ता है। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘टीबी मुक्त भारत अभियान’ की शुरुआत की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि दुनिया ने टीबी को खत्म करने के लिए 2030 तक समय तय किया है, लेकिन भारत ने अपने लिए यह लक्ष्य 2025 तय किया है। पिछले साल वर्ल्ड टीबी समिट में मोदी ने फिर इसी बात को दोहराया था कि ‘टीबी खत्म करने का ग्लोबल टारगेट 2030 है।
भारत फ़िलहाल साल 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। दुनिया से पांच साल पहले। इतने बड़े देश ने इतना बड़ा संकल्प अपने देशवासियों के भरोसे लिया है।’ भारत के लिए इतना बड़ा ऐलान इसलिए भी अहम है क्योंकि डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज भारत में ही हैं। 2025 में अब साल भर का ही वक्त बचा है। ऐसे में क्या इतने कम वक्त में हजारों साल पुरानी इस बीमारी से पीछा छुड़ा पाना संभव है? आंकड़े बताते हैं कि इस लक्ष्य को पाने में भारत को अभी शायद और वक्त लग जाए।
भारत में रोज़ाना क़रीब छह हज़ार से ज़्यादा लोग टीबी की चपेट में आते हैं और एक चौथाई यानी एक हज़ार मरीज़ परलोक सिधार जाते हैं। दुनिया में लगभग 10 करोड़ लोग टीबी से पीड़ित है। भारत हर साल लाखों लोगों की टीबी और उससे जनित बीमारियों मौत हो जाती है। यह हाल तब है जब दावा किया जाता है कि टीबी अब लाइलाज नहीं रही। जो बीमारी लाइलाज नहीं है, उससे इतने ज़्यादा लोगों की मौत हैरान करती है। टीबी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ही 24 मार्च को टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1882 में इसी दिन जर्मन जीवाणुविज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता सर रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले टीबी के बैक्टीरिया के बारे में बताया था।
डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, हर साल दुनिया में टीबी के जितने मरीज सामने आते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा मामले भारत में होते हैं। डब्ल्यूएचओ की ‘ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023’ की मानें तो 2022 में टीबी के 27% मामले भारत में सामने आए थे। यानी, 2022 में दुनिया में मिलने वाला टीबी का हर चौथा मरीज भारतीय था। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया और फिर तीसरे नंबर पर चीन है। 2023 में दुनियाभर में 75 लाख से ज्यादा लोग टीबी की चपेट में आए। इस दौरान भारत में 22.3 लाख लोग टीबी से पीड़ित हुए।
भारत में टीबी मरीज़
• 2021 – 28.2 लाख
• 2022 – 24.2 लाख
• 2023 – 22.3 लाख
भारत के बाद सबसे ज्यादा 10 फ़ीसदी मरीज इंडोनेशिया और फिर 7.1 फ़ीसदी चीन में थे। इनके बाद फिलिपींस में 7 फ़ीसदी, पाकिस्तान में 5.7 फ़ीसदी, नाइजीरिया में 4.5 फ़ीसदी, बांग्लादेश में 3.6 फ़ीसदी और कॉन्गों में 3 फ़ीसदी मरीज सामने आए।
इस बीमारी को क्षय रोग और तपेदिक रोग भी कहा जाता है। टीबी आनुवांशिक रोग नहीं है। यह बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है। टीबी घातक संक्रामक बीमारी है जो आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है। हालांकि यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। टीबी के बैक्टीरिया हवा के ज़रिए फैलते हैं। दरअसल, टीबी मरीज़ खांसी, छींक या किसी अन्य प्रकार से अपने बैक्टीरिया हवा में छोड़ते हैं जो आस-पास होने वाले व्यक्ति को संक्रमित करते हैं और सांस के ज़रिए उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे छुटकारा पाने का तरीक़ा इसका पूरा इलाज है और सही उपचार न मिल पाने से 50 फ़ीसदी से ज़्यादा लोगों की मोत हो जाती है।

क्या है टीबी?
टीबी पहले राजाओं महाराजाओं का रोग कहा जाता था, क्योंकि पहले यह बड़े लोगों को होता था। धीरे-धीरे यह ग़रीबों की बीमारी बन गई, क्योंकि संपन्न लोग तो इलाज करवा लेते हैं, लेकिन ग़रीबों को सही इलाज नहीं मिल पाता। घातक संक्रामक रोग टीबी के बैक्टीरिया ज़्यादातर फेफड़ों में ही पाए जाते हैं। लेकिन ये ख़तरनाक बैक्टीरिया आंते, मस्तिष्क, हड्डियों, जोड़ों, गुर्दे, त्वचा, दिल को ग्रसित कर सकते हैं। कह सकते हैं, टीबी बैक्टीरिया शरीर के हर अंग को प्रभावित करते हैं।
टीबी के लक्षण
• तीन-चार हफ़्ते से अधिक लगातार खांसी आना।
• बलगम के साथ खून आना
• खासतौर पर शाम को बढ़ने वाला बुखार होना।
• पूरे सीने में लगातार तेज़ दर्द होना
• मरीज़ का वज़न का घटना
• अचानक भूख में लगना बंद हो जाना
• फेफड़ों में इंफेक्शन बहुत ज़्यादा होना
• सांस लेने में काफी दिक़्क़त होना
टीबी से बचाव
• बच्चे को एक महीने का हाने से पहले टीबी का टीका लगवाना।
• खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना।
• मरीज़ को जगह-जगह थूकने से रोकना।
• इलाज का कोर्स पूरा करना।
• अल्कोहल और धूम्रपान से परहेज करना।
• बहुत ज़्यादा श्रम वाला काम बिल्कुल न करना
कैसे होता है टीबी संक्रमण?
टीबी रोगियों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि टीबी रोगियों के कफ, छींक, खांसी, थूक और उनके सांस से बैक्टीरिया पहले वातावरण में प्रवेश करते हैं और फौरन आसपास मौजूद व्यक्ति के सांस के साथ उसके फेफड़े तक पहुंच जाते हैं। इस तरह टीबी मरीज़ों के संपर्क में आने के कारण अच्छा ख़ासा स्वस्थ आदमी भी भी आसानी से टीबी का शिकार हो जाता है। किसी टीबी मरीज़ के के कपड़े पहनने, उससे हाथ मिलाने या उसे छूने से टीबी नहीं फैलता।
डॉक्टरों का कहना है कि जब भी टीबी के बैक्टीरिया सांस के जरिए दूसरे व्यक्ति के फेफड़े तक पहुंचते हैं तब वे कई गुना बढ़ जाते हैं। टीबी के बैक्टीरिया फेफड़े को संक्रमित कर देते हैं। कभी-कभी हट्टे-कट्टे व्यक्ति का मज़बूत इम्यून सिस्टम इन्हें रोक लेता है, लेकिन ज़्यादातर मामले में ये बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं और मरीज़ काइम्यून सिस्टम कमज़ोर कर देते हैं। टीबी का संक्रमण तीन चरणों में होता है।
प्रथम चरण: टीबी की पहली अवस्था में मरीज़ के पसलियों में दर्द होता है।त उसके हाथ-पांव अकड़ जाते हैं। उसके पूरे बदन में हल्की टूटन सी हमसूस होती है और मरीज़ को लगातार बुखार बना रहता है। इस अवस्था में मर्ज का पता लगाने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
द्वितीय चरण: टीबी की दूसरी अवस्था में मरीज़ की आवाज़ भारी या मोटी हो जाती है। उसके पेट में दर्द होता है। इसके अलावा कमर दर्द और बुखार भी होता है। इस अवस्था में अगर मर्ज का पता लग जाए तो आसानी से इलाज हो जाता है।
तृतीय चरण: टीबी की तीसरी अवस्था में रोगी को बहुत तेज़ बुखार होता है। उसे लगातार तेज़ खांसी आती है। खांसी बहुत कष्टदायक होती है। मरीज़ को कफ के साथ खून भी आने लगता है, जिससे उसका शरीर बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। टीबी की यह अवस्था सीरियस होती है।
कैसे कराएं जांच?
टीबी होने की आशंका होने पर जांच कराने के कई तरीक़े हैं। सबसे पहले सीने का का एक्स रे करवाते हैं। उसके बाद कफ यानी बलगम की जांच करवाने के बाद कई बार डॉक्टर स्किन के टेस्ट की भी सलाह देते हैं। आजकल टीबी का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीक आईजीएम से हीमोग्लोबीन का भी जांच होने लगा है। हर सरकारी अस्पतालों में सभी जांच मुफ़्त में होती है।
टीबी का ट्रीटमेंट
आजकल तो टीबी का सहज़ इलाज उपलब्ध है। डॉक्टरों का कहना है कि टीबी मरीज़ कोर्स करके इस बीमारी से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। सरकारी के डॉट्स सेंटर देश भर में हैं, जहां टीबी के मुफ़्त इलाज होता है। इन केंद्रों मरीज़ को क्लिनिक में ही दवाई खिलाई जाती है, ताकि उपचार में मरीज़ की ओर से कोताही न बरती जाए। जिन्हें टीबी है, उन्हें इन केंद्रों पर ज़रूर जाना चाहिए।
खाना-पीना कैसा हो
डॉंक्टरों का कहना है कि टीबी के रोगदियों को हाई प्रोटीन वाले संतुलित आहार देने चाहिए। खाने में किसी तरह के परहेज की ज़रूरत नहीं है। बस उका भोजन पौष्टिकत तत्वों से भरपूर होना चाहिए। दूध, अंडे, मुर्गा, मांस, मछली में ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसलिए मरीज़ो को भोजन में इनकी बहुतायत होनी चाहिए। मरीज़ को अखरोट, लहसुन, लौकी, हींग, आम का रस, तुलसी, देसी शक्कर, बड़ी मुनक्का और अंगूर भी देना बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अगर सामान्य व्यक्ति को एक ग्राम प्रोटीन डाइट की सलाह दी जाती है तो टीबी के मरीज को 1।5 ग्राम प्रोटीन चाहिए।
बच्चों में टीबी
मौजूदा समय में बड़ों के साथ बच्चे भी टीबी के शिकार होने लगे हैं। बालरोग कंसल्टेंट्स का मानना है, ‘समाज में सामाजिक और आर्थिक गिरावट तो इसकी बड़ी वजह है। बदली जीवनशैली और खान-पान की वजह से भी बच्चों में टीबी की समस्या आम होती जा रही है। आजकल बच्चे जंक फूड खूब खाते हैं, जिससे उनके शरीर को पौष्टिक तत्व कम मिलते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ गई है।
अमिताभ को भी टीबी!
बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता अमिताभ बच्चन टीबी पर जागरूकता अभियान से जुडे हुए हैं। टीबी से पीड़ित लोगों को राहत दिलाने के लिए शुरू किए गए अभियान से अमिताभ को बतौर एंबैसेडर जोड़ा गया है। बिग बी ने ‘टीबी फ़्री इंडिया’ की प्रेस वार्ता में अपने एक अनुभव को साझा करते हुए बताया कि सन् 2000 में अचानक पता चला कि उन्हें टीबी है। बहराहाल इलाज से वह ठीक हो गए, लेकिन भारी मात्रा में दवाइयों की खुराक लेनी पड़ी थी। बिग बी ने कहा, “अगर टीबी मुझे हो सकती है तो किसी को भी हो सकती है। अभी भी भारत में टीबी को एक अवांछनीय बीमारी माना जाता है और लोग इससे डरते हैं।” अमिताभ ने बताया कि कैसे टीबी का रोगी आराम से काम कर सकता है, शर्त सिर्फ़ इतनी है कि दवा की गोलियां लेने में कोई कोताही न बरती जाए।
अमीरों की बीमारी
अमिताभ ने कहा, “लोग इस बीमारी से घबराते हैं, टीबी से फ़िल्मों में लोगों को मरते देखकर लोगों को असल ज़िंदगी में भी इससे डरते देखा जा सकता है, लेकिन यह लाइलाज नहीं है।” टीबी फ़्री इंडिया के आंकड़ों पर नज़र डाले तो कभी महानगरों में होने वाली यह बीमारी अब तेज़ी से मुंबई की झुग्गी बस्तियों में फैल रही है। टीबी के मरीजों के साथ होने वाले बुरे बर्ताव के बारे में अमिताभ कहते हैं, “टीबी प्रभावित लोगों के साथ दुर्भाग्यवश भेदभाव होता है, खासकर विवाहित महिलाएं इसका शिकार होती हैं, या लड़कियों को शादी के प्रस्ताव मिलने में दिक्कत होती है। अगर शादी हो गई तो घर से बाहर कर देते हैं। समाज में फैली इस कुप्रथा को हम इस अभियान से ठीक कर सकते हैं, जैसे उचित दवा से टीबी को।”
टीबी का घरेलू उपचार
लहसुन
लहसुन में सल्फुरिक एसिड होता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो टीबी के बैक्टीरिया और कीटाणुओं का नाशकर देता है। लहसुन इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। इसे भूनकर या पकाकर या फिर कच्चा ही खाना चाहिए। इसे खाने का तरीक़ा है कि लहुसन की 10 कलियों को एक कप दूध में उबाल लें और उबली हुई कलियों को चबाकर खा लें और ऊपर से दूध पी जाएं। ऐसा दो हफ़्ते तक करें। इस दैरान पानी ना पीएं वर्ना लहसुन असर नहीं करेगी।
आंवला
आंवला अपने सूजन विरोधी एवं ऐंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए मशहूर है। आवला के पोषक तत्व शरीर की प्रक्रियाओं को सही ढंग ढंग से चलाने की ताक़त होती है। चार या पांच आंवले का बीज निकाल कर उनका जूस बनाकर उसमें एक चम्मच शहद मिलाकर रोज़ाना खाली पेट पीना चाहिए। टीवी के रोगी के लिए इसे अमृत माना गया है। कच्चा आंवला या उसका पाउडर भी लाभकारी होता है। यह शरीर को कई तरह के पोषण पहुंचा कर उसे मजबूती प्रदान करता है।
सहिजन
सहिजन टीबी पैदा करने वाले बैक्टीरिया से मुक्ति दिला सकता है। सहिजन फेफड़े की सूजन को घटाता है, जिससे संक्रमण से राहत दिलाती है। सहिजन की मुठ्ठीभर पत्तियां एक कप पानी में पांच मिनट तक गरम करके फिर ठंडा कर ले। उसमें नींबू, नमक और मिर्च निचोड़कर रोगी को पीने के लिए दें। इसका सेवन रोज़ाना सुबह खाली पेट करना चाहिए। इसके अलावा उबाली हुई सहिजन का रोज़ाना सेवन करने सेटीबी के बैक्टीरिया मर जाते हैं।
केला
पौषक तत्वों से परिपूर्ण केले में बहुत मात्रा में कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम में टीबी के रोगियों का इम्यून सिस्टम मज़बूत करने की क्षमता होती है। एक पका कला मसलकर उसमें एक कप नारियल पानी,आधा कप दही और एक चम्मच शहद मिलाकर दिन में दो बार लेने से टीबी रोग ठीक हो जाता है। इसके अलावा कच्चे केले का जूस एक गिलास मात्रा में रोज सेवन करें। टीबी मरीज़ को एक गिलास कच्चे केले का जूस रोज़ाना सेवन करना चाहिए।
संतरा
फेफड़े पर संतरे का अल्कली (क्षारीय) प्रभाव फ़ायदेमंद होता है। यह इम्यून सिस्टम को बल देने वाला है। कफ सारक है याने कफ को आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। एक गिलास संतरे के रस में चुटकी भर नमक, एक बड़ा चम्मच शहद अच्छी तरह मिलाकर सुबह और शाम दोनों समय पीना चाहिए। इससे टीबी रोग के वायरस मर जाते हैं।
सीताफल
टीबी से छुटकारा पाने के लिए सीताफल को मैश कर लें और एक कप पानी में 25 किशमिश डालकर साथ ही सीताफल का गूदा उसमें डाल दें। उस मिश्रण को अच्छी तरह उबाल लें। पानी जल जाने का बाद इसे छान लें और इसमें इलायची पाउडर और साथ ही दो छोटे चम्मच चीनी मिलाएं। ठंडा होने पर इसका रोज़ाना दिन में दो बार सेवन करें। बहुत जल्दी फायदा होगा।
काली मिर्च
काली मिर्च शरीर को कई रोगों से राहत दिलाने में मदद करती हैं। यह फेफड़े की सफाई करती है और टीबी की वजह से होने वाले दर्द को दूर करती है। टीबी की बीमारी से राहत पाने के लिए काली मिर्च के 10-15 दाने को घी में फ्राई करने के बाद चुटकी भर हींग पाउडर डालकर मिक्स कर लें और ठंडा होने के बाद मिश्रण को तीन भागों में बांटकर एक घंटे के बाद इसका सेवन करें, इससे शर्तिया आराम मिलेगा।
पुदीना
पुदीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है इसमें ऐसे एंटी बैक्टीरियल गुण होते है जो शरीर को कफ से निजात दिलाने में मदद करते है। यह फेफडे़ को भी ख़राब होने से बचाता है। आधा कप गाजर के जूस में, एक चम्मच पुदीने का रस, दो चम्मच शहद और दो चम्मच शुद्ध सिरका मिलाएं। इस मिश्रण को तीन भाग में बांट लें और हर एक घंटे में पीएं। टीबी की बीमारी से राहत पाने के लिए पूदीना फायदेमंद साबित होता है।
ग्रीन टी
ग्रीन टी पीना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसे पानी में अच्छी तरह से उबाल कर इसका सेवन करें। यह टीबी बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया का खात्मा करते हैं यह शरीर की इम्यून सिस्टम क्षमताओं को बढ़ाती भी है। ग्रीन टी पीने से टीबी पैदा करने वाले बैक्टीरिया का ख़तरा कम हो जाता है।
दूध
दूध पीना हमारी सेहत के लिए लाभकारी होता है, दूध से मिलने वाले कैल्शियम से इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है और साथ ही हमारे शरीर की हड्डियों मजबूत बनती है। टीबी होने पर हड्डियों को नुकसान पहुंचाने वाले संक्रमण से बचने के लिए दूध का सेवन करना लाभकारी साबित होता है।
लेखक – हरिगोविंद विश्वकर्मा